UDAY PRAKASH
Wednesday, March 2, 2011
दो साल पहले की एक पोस्ट, जिसे मैने 'डैशबोर्ड' के आर्काइव से निकाला
(यह पोस्ट मैने दो साल पहले लिखी थी। आज अचानक ही अपने ब्लाग के 'डैशबोर्ड' की सफाई के लिए गया तो यह वहां मिला । ..अक्सर ऐसे पोस्ट को लगाया नहीं जाना चाहिये। किसी खास मूड और हताशा के पलों में वे पैदा होते हैं। ..लेकिन फिर भी इसे मैं लगा रहा हूं । इसे स्वस्थ ढंग से लिया जाय और जो हमेशा सत्ता, संपर्क, जोड-तोड, गुट्बाजी आदि में मुब्तिला रहते हैं, वे एक बार ज़रूर सोचें कि उनकी इन गतिविधियों से अकेला उदय प्रकाश ही नहीं, हज़ारों-लाखों लेखक प्रभावित-प्रताडित होते रहते हैं। कई तो गुमनामी और वंचना के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते हैं।....
यह पोस्ट मैं इसलिए भी लगा रहा हूं कि अब हालात और बिगड चुके हैं...! हांलाकि दूसरी ओर एक ऐसी विराट जागृति भी क्षितिज में उभरती दिखाई दे रही है, जो भ्रष्टाचार, निरंकुशता, झूठ, जाति-नस्लवाद आदि को समूल उखाड फेंकने के लिए मिस्र, लीबिया से लेकर सारी दुनिया में अपनी मौज़ूदगी दर्ज करा रही है।
बस इसे पढिये और इसे लेकर अगर जातिवादी-सत्तापरस्त-राजनीतिक गुटों ने तूल बनाना शुरू किया तो अपने इस लेखक के साथ रहिए। अपनी भाषा, अपने समाज, अपने देश को स्वतंत्र, समतामूलक, बिरादराना और आधुनिक बनाने के लिए लंबी लडाई लडें।
(पुरानी पोस्ट : असंपादित )
मैंने आख़िरी पोस्ट ४ जुलाई को लिखी थी और आज २७ नवम्बर हैं|.....बीच का समय यात्राओं और भटकावों से भरा हुआ है| थकान, उलझनों, खुशियों और तनावों में डूबता-उतराता |
जब मैं दिल्ली से जा रहा था , रास्ते में पत्नी कुमकुम ने कहा आपको याद है आज ९ जुलाई है| इसी तारीख को ३१ वर्ष पहले हमने विवाह किया था|
हमारे सामने सड़क थी| एक हज़ार पचास किलोमीटर आगे हमें अपने गांव जाना था | मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़ का सिवान | हम अपना ठिकाना खोज रहे थे | कहीं बसने की कोशिश|
यह पोस्ट मैं इसलिए भी लगा रहा हूं कि अब हालात और बिगड चुके हैं...! हांलाकि दूसरी ओर एक ऐसी विराट जागृति भी क्षितिज में उभरती दिखाई दे रही है, जो भ्रष्टाचार, निरंकुशता, झूठ, जाति-नस्लवाद आदि को समूल उखाड फेंकने के लिए मिस्र, लीबिया से लेकर सारी दुनिया में अपनी मौज़ूदगी दर्ज करा रही है।
बस इसे पढिये और इसे लेकर अगर जातिवादी-सत्तापरस्त-राजनीतिक गुटों ने तूल बनाना शुरू किया तो अपने इस लेखक के साथ रहिए। अपनी भाषा, अपने समाज, अपने देश को स्वतंत्र, समतामूलक, बिरादराना और आधुनिक बनाने के लिए लंबी लडाई लडें।
सच मानिये इस सब में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बल्कि यह एक जोखिम ही है, जिसे मैं फिर मोल ले रहा हूं। )
(पुरानी पोस्ट : असंपादित )
मैंने आख़िरी पोस्ट ४ जुलाई को लिखी थी और आज २७ नवम्बर हैं|.....बीच का समय यात्राओं और भटकावों से भरा हुआ है| थकान, उलझनों, खुशियों और तनावों में डूबता-उतराता |
जब मैं दिल्ली से जा रहा था , रास्ते में पत्नी कुमकुम ने कहा आपको याद है आज ९ जुलाई है| इसी तारीख को ३१ वर्ष पहले हमने विवाह किया था|
हमारे सामने सड़क थी| एक हज़ार पचास किलोमीटर आगे हमें अपने गांव जाना था | मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़ का सिवान | हम अपना ठिकाना खोज रहे थे | कहीं बसने की कोशिश|
फिर तीन महीने सात दिन छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में ही बीते | दुर्ग, रायपुर, अम्बिकापुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर ..... और उस इलाके के कई गांव | एक दूसरी उपत्यका| एक और उपग्रह | एक दूसरा हिन्दुस्तान |
जिस दिन मैं वहां अपने गांव पहुचा , उसके अगले दिन १३ जुलाई को ठूनू की मृत्यु हुई | पिछले साल मैं उसे एक चश्मा दे आया था | वह खुश था और वह और जीना चाहता था | लेकिन ७० की उम्र में वह सुबह कुयें के जगत पर दातून करते हुए मर गया |
गांव में हल्ला था कि वह पंचक में मरा है | और अब वह अपने साथ इस गांव के पांच जीवित लोगों को और ले जायेगा |
गांव ऐसे ही भय और अंधविश्वास में जीते हैं | आज भी |
गांव में हल्ला था कि वह पंचक में मरा है | और अब वह अपने साथ इस गांव के पांच जीवित लोगों को और ले जायेगा |
गांव ऐसे ही भय और अंधविश्वास में जीते हैं | आज भी |
लेकिन यह भय सच था |
सत्रह दिनों में मेरे गांव और उसके आस-पास के टोलों में छः लोगों की मृत्यु हुई | समीरा ने आत्महत्या की| सौरहा टोला की एक औरत रात में सांप काटने से मरी | दो लोग बुढापे के कारण मरे | लेकिन अगर उन्हें ठीक खाना मिलता और ज़रूरी दवाईयां, तो वे दस-पन्द्रह साल और जी सकते थे | दो मौतें मैलेरिया से हुई | गाजर घास और लन्टिना जैसे खर-पतवारों के बेतहाशा फैलाने से घातक मैलेरिया उस पूरे इलाके में बहुत फैल रहा है | नए किस्म के मच्छर उन्ही की जड़ों में पनपते हैं , ऐसा लोगों ने बताया |
लेकिन वहां की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है -गरीबी |
सत्रह दिनों में मेरे गांव और उसके आस-पास के टोलों में छः लोगों की मृत्यु हुई | समीरा ने आत्महत्या की| सौरहा टोला की एक औरत रात में सांप काटने से मरी | दो लोग बुढापे के कारण मरे | लेकिन अगर उन्हें ठीक खाना मिलता और ज़रूरी दवाईयां, तो वे दस-पन्द्रह साल और जी सकते थे | दो मौतें मैलेरिया से हुई | गाजर घास और लन्टिना जैसे खर-पतवारों के बेतहाशा फैलाने से घातक मैलेरिया उस पूरे इलाके में बहुत फैल रहा है | नए किस्म के मच्छर उन्ही की जड़ों में पनपते हैं , ऐसा लोगों ने बताया |
लेकिन वहां की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है -गरीबी |
बिजली वहां कुल मिलाकर ४-५ घंटे के लिए आती है | मोबाइल के नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते | मेरा 'एयरटेल' गूंगा-बहरा हो चुका था |
जब ४ जुलाई को दिल्ली छोड़ कर हम लोग जा रहे थे तब सेंसेक्स २०,००० की गगन चुम्बी उंचाइयां पार कर चुका था | संसद में नोटों की करोडों की गड्डियां बटते हमने वहां कसबे के एक दोस्त के घर पर टी वी पर देखा | यह किसी दूसरी दुनिया से आने वाली खबरें होती हैं | उस दुनिया से जहां से राजनीति और ठेकेदार और बंदूकें आती हैं | जहां से हिंसा और उत्पीडन के सामान आते हैं |
ठूनू , समीरा, सुखानिया सभी की कथाएं हैं | उन सभी का जीवन हमारे समय का ही आख्यान था | मोहनदास की तरह, या टेपचू और वाकणकर की तरह | शायद हम सबकी तरह | पूंजी और राजनीतिक सत्ता के उपनिवेशों में अपनी अपनी त्रासदियां और दुखांत रचते हुए|
मोहनदास १७ -१९ जुलाई को ओसियान फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाई गयी | फ़िल्म के प्रोड्यूसर यानी उत्तर प्रदेश के राज्य परिवहन के अफसर , जो हिन्दी की एक साहित्यिक पत्रिका भी निकालते हैं, सवर्ण हिन्दी के उस तथाकथित वामपंथी गुट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका हर बडे पुलिस अधिकारी, आई.इ.एस. अफसर, मंत्री आदि से गहरा अनैतिक और बेशर्म संबंध है| अपने ३२ साल के दिल्ली के जीवन में मैंने जिसके किसी भी मेंबर को 'बेरोजगार' कभी नहीं देखा| अखबारों, कारपोरेट घरानों, सरकारी संस्थानों में जो, तमाम लाभ के पद और पुरस्कार बटोरता उसी तरह टहलता है, जैसे ये सभी उसके फ़्लैट के टायलेट हों|
वह हर जगह मौज़ूद है। वह सबसे ऊंची जातियों का है।
श्रम से अधिक जुगाड और 'लायज़निंग' पर वह निर्भर है। लेकिन वह नाजिम हिकमत, ब्रेख्त, नेरूदा. लोर्का, पाश, फैज़ और तमाम क्रांतिकारी कवियों लेखकों के नाम ऐसे लेता है, जैसे वे उसकी निजी जागीर हों|
ऐसे लेखकों आप अकेला कभी नहीं देखेंगे। वह गिरोहबंद है। चोम्स्की जिसे 'क्लेप्टोक्रेट' कहते हैं, यानी 'लुटेरा-माफिया समूह', यह वही है। यह किसी को भी हिंदी में तबाह करने की ताकत रखता है।
लेकिन इसे परास्त करना इसलिए ज़रूरी है क्य़ोंकि बिना इसके अपनी भाषा को स्वतंत्र और आधुनिक नहीं किया जा सकता।
वह हर जगह मौज़ूद है। वह सबसे ऊंची जातियों का है।
श्रम से अधिक जुगाड और 'लायज़निंग' पर वह निर्भर है। लेकिन वह नाजिम हिकमत, ब्रेख्त, नेरूदा. लोर्का, पाश, फैज़ और तमाम क्रांतिकारी कवियों लेखकों के नाम ऐसे लेता है, जैसे वे उसकी निजी जागीर हों|
ऐसे लेखकों आप अकेला कभी नहीं देखेंगे। वह गिरोहबंद है। चोम्स्की जिसे 'क्लेप्टोक्रेट' कहते हैं, यानी 'लुटेरा-माफिया समूह', यह वही है। यह किसी को भी हिंदी में तबाह करने की ताकत रखता है।
लेकिन इसे परास्त करना इसलिए ज़रूरी है क्य़ोंकि बिना इसके अपनी भाषा को स्वतंत्र और आधुनिक नहीं किया जा सकता।
बहरहाल, 'मोहन दास' फिल्म का यह प्रोड्यूसर पिछले कुछ वर्ष किसी संगीन आरोप में निलंबित भी रह चुका है| इसी प्रोड्यूसर और मेरे कई डाक्युमेंटरीज में कैमरामैंन रह चुके और अब मेरे ही कारण पहली बार किसी फ़िल्म के निर्देशक बने व्यक्ति ने मुझे निमंत्रित नहीं किया था |
वजह ?
मैं इसे समझ पाने में हमेशा असफल रहा करता हूँ|
हद तो यह थी कि अपने कई इंटरव्यू में निर्देशक ने कहानी को अपनी मौलिक कल्पना घोषित किया था | ये सारे लिंक नेट पर उपलब्ध हैं|
लेकिन पता चला कि तमाम युवाओं ने अपने ब्लॉग पर और कई समीक्षाओं में इन सब कोशिशों की धज्जियां बिखेर दीं| अगर 'मोहन दास' पहले से ही इतना लोकप्रिय न हो गया होता, उसके इतने अनुवाद और इतने मंचन न हुए होते, तो हिंदी साहित्य का एक पूरा गिरोह इस तैयारी में था कि इसे विवादित कर दिया जाय|
वे ऐसा कई बार कर चुके हैं..! मेरी रचनाओं में व्यक्तियों की खोज, उसे 'नक़ल' आदि कहना और अपने संपर्क के जरिये अखबारों में अभियान चलाना..! यह एक डरावना आतंकवाद है| एक तरह का फासीवाद|
लेकिन हर बार जनता ने, तमाम भाषाओँ के बौद्धिकों-रचनाकारों ने हस्तक्षेप किया है| और हम बचे हैं|
वे मेरे पाठक ही हैं...और वे सारे युवा जो मेरी अस्मिता को बचाए हुए हैं..!
हर बार, अचानक वे कहीं से आते हैं और मुझे अंधेरों में से निकाल लेते हैं..!
पता चला 'जनसत्ता' में कुंवर नारायण जी ने भी लिखा कि कि जब ओसियान में 'मोहन दास' दिखाई जा रही थी, तो उदय प्रकाश कहाँ थे? कहीं उनके साथ फ़िल्म बनाने वालों ने वही तो नहीं किया, जो इस फ़िल्म में 'मोहन दास' के साथ किया गया?
उनका मैं कृतज्ञ हूँ| 'आत्मजयी' जब अपने बचपन में, गाँव में पढी थी, उसके बाद ही कठोपनिषद खरीद लाया था| उनके अन्दर कोई एक गहरी नैतिक करुना है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है|
वजह ?
मैं इसे समझ पाने में हमेशा असफल रहा करता हूँ|
हद तो यह थी कि अपने कई इंटरव्यू में निर्देशक ने कहानी को अपनी मौलिक कल्पना घोषित किया था | ये सारे लिंक नेट पर उपलब्ध हैं|
लेकिन पता चला कि तमाम युवाओं ने अपने ब्लॉग पर और कई समीक्षाओं में इन सब कोशिशों की धज्जियां बिखेर दीं| अगर 'मोहन दास' पहले से ही इतना लोकप्रिय न हो गया होता, उसके इतने अनुवाद और इतने मंचन न हुए होते, तो हिंदी साहित्य का एक पूरा गिरोह इस तैयारी में था कि इसे विवादित कर दिया जाय|
वे ऐसा कई बार कर चुके हैं..! मेरी रचनाओं में व्यक्तियों की खोज, उसे 'नक़ल' आदि कहना और अपने संपर्क के जरिये अखबारों में अभियान चलाना..! यह एक डरावना आतंकवाद है| एक तरह का फासीवाद|
लेकिन हर बार जनता ने, तमाम भाषाओँ के बौद्धिकों-रचनाकारों ने हस्तक्षेप किया है| और हम बचे हैं|
वे मेरे पाठक ही हैं...और वे सारे युवा जो मेरी अस्मिता को बचाए हुए हैं..!
हर बार, अचानक वे कहीं से आते हैं और मुझे अंधेरों में से निकाल लेते हैं..!
पता चला 'जनसत्ता' में कुंवर नारायण जी ने भी लिखा कि कि जब ओसियान में 'मोहन दास' दिखाई जा रही थी, तो उदय प्रकाश कहाँ थे? कहीं उनके साथ फ़िल्म बनाने वालों ने वही तो नहीं किया, जो इस फ़िल्म में 'मोहन दास' के साथ किया गया?
उनका मैं कृतज्ञ हूँ| 'आत्मजयी' जब अपने बचपन में, गाँव में पढी थी, उसके बाद ही कठोपनिषद खरीद लाया था| उनके अन्दर कोई एक गहरी नैतिक करुना है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है|
खैर, अगर आप एक लेखक, कलाकार और कवि का जीवन जीते हैं तो अन्यायी और भ्रष्ट ताकतें आपके साथ वही व्यवहार करती है , जो उन्होंने 'मोहनदास' के साथ किया, या जो वे अपने समय के अशक्त, गरीब, मेहनतकशों और नागरिकों के साथ करती हैं |
ओसियान में फ़िल्म के क्रेडिट के डिस्प्ले के साथ भी ऐसा ही हुआ |
ओसियान में फ़िल्म के क्रेडिट के डिस्प्ले के साथ भी ऐसा ही हुआ |
जिस दिन दिल्ली में ओसियन फ़िल्म फेस्टिवल में मोहनदास फ़िल्म दिखाई जा रही थी उस दिन मैं अनूपपुर की सब्जी मंडी में दोअपहर और रात के खाने के लिए सब्जी खरीद रहा था| तभी मोबाइल बजा| उधर से अजीत कौर बोल रहीं थीं| पंजाबी की विख्यात लेखिका, सार्क लेखक संगठन की संयोजिका और अकादमी आफ फाइन आर्ट्स की संचालक|
दिल्ली में एक ऐसी उपस्थिति, जिनसे मैं शायद ही कभी मिलता होउं, लेकिन जब भी, जहां कहीं भी मेरा लिखा कुछ छापता है, उनका फोन ज़रूर आता है| आत्मीयता से भरा| दुलारता-सा| प्रोत्साहित करता|
वही आवाज़ थी| 'उदय जी आप कहां हैं?...मैं अभी मोहन दास देख कर निकली हूं| पूरे अपने जीवन में मैं चार बार रोई थी, आज इस फ़िल्म में सात बार रोई हूँ...!'
..उनकी आवाज़ में वही वत्सलता है|
'मैं अपने गाँव में हूँ और इस वक्त मोहन दास मेरे साथ ही है|' मैं अपनी भावुकता को संभालते हुए कहता हूँ|
थोड़ी ही देर में फोन डेड हो जाता है| ऐसा ही होता है यहाँ| बात पूरी भी नहीं हो पाई थी|
मैंने लगभग दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया है|
ज़हालत है, अगर आप ताकतवर नहीं हैं, किसी गिरोह में नहीं हैं, किसी अफसर, मंत्री, व्यावसायिक घराने, माफिया के सदस्य नहीं हैं| आश्चर्य है की यहाँ शायद ही कोई यह सुनने के लिए तैयार हो कि २५ साल बिना किसी नौकरी के रहना कितना मुश्किल और जानलेवा है|
वे सब मुस्कुराहटों से भरे, संतुष्ट, अघाए और आर्थिक रूप से सुरक्षित लोग हैं|
दसवीं दर्जे की शिक्षा है लेकिन वि.वि. और कालेजों के प्रोफेसरों की नियुक्ति करते हैं| मुश्किल से ग्रेजुएट हैं लेकिन केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के एकेडमिक कौंसिल के सदस्य हैं|
वे मेरे समकालीन हैं| वे सब महान हैं| खैर!
यहाँ गाँव में स्थितियाँ विकट हैं| पहले से भी बदतर|
ग्रामपंचायतों में इतना भ्रष्टाचार और इतनी हिंसा की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी| खदानों में नंबर दो का अवैध उत्खन हर जगह चल रहा है और इसमें समूचा राजनीतिक-प्रशासनिक तंत्र शामिल है|
मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो कहीं मुझे भी 'नक्सल' न घोषित कर दिया जाए| अगर ऐसा किया गया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने आप को वामपंथी कहने वाले सवर्ण हिन्दी लेखक, जो अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े 'लेखक संगठनों' को चलाते हैं और राजधानियों में रहते हुए अपने बेटे, दामाद, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, जाती-बिरादरी को हर सरकारी संस्थान में फिट कराते रहते हैं और जो अतीत की तमाम महा-वृत्तांतों ..१८५७, गांधी, भगत सिंह, मार्क्स-लेनिन वगैरह का नाम लेते रहते हैं, वे सब मेरी यंत्रणा में सत्ता के और मददगार होंगें|
उनके तो ऐसे बड़े-बड़े पुलिस अफसरों से करीबी रिश्ते हैं, जिनके अध्: पतन के किस्से मैं सुनता रहता हूँ| उन सबको वे मुक्तिबोध, रेणु अदि बताते रहते हैं...!ओह!
लगता है मैं इस पोस्ट को लिख नहीं पाउँगा ..! मैं अपनी उँगलियों को, जो की-बोर्ड पर चल रही हैं..अपने दिमाग से अलग नहीं कर पा रहा हूँ ..!
या हज़रत ...औलिया ...! हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे...! सच कहने की शक्ति..!
दिल्ली में एक ऐसी उपस्थिति, जिनसे मैं शायद ही कभी मिलता होउं, लेकिन जब भी, जहां कहीं भी मेरा लिखा कुछ छापता है, उनका फोन ज़रूर आता है| आत्मीयता से भरा| दुलारता-सा| प्रोत्साहित करता|
वही आवाज़ थी| 'उदय जी आप कहां हैं?...मैं अभी मोहन दास देख कर निकली हूं| पूरे अपने जीवन में मैं चार बार रोई थी, आज इस फ़िल्म में सात बार रोई हूँ...!'
..उनकी आवाज़ में वही वत्सलता है|
'मैं अपने गाँव में हूँ और इस वक्त मोहन दास मेरे साथ ही है|' मैं अपनी भावुकता को संभालते हुए कहता हूँ|
थोड़ी ही देर में फोन डेड हो जाता है| ऐसा ही होता है यहाँ| बात पूरी भी नहीं हो पाई थी|
मैंने लगभग दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया है|
ज़हालत है, अगर आप ताकतवर नहीं हैं, किसी गिरोह में नहीं हैं, किसी अफसर, मंत्री, व्यावसायिक घराने, माफिया के सदस्य नहीं हैं| आश्चर्य है की यहाँ शायद ही कोई यह सुनने के लिए तैयार हो कि २५ साल बिना किसी नौकरी के रहना कितना मुश्किल और जानलेवा है|
वे सब मुस्कुराहटों से भरे, संतुष्ट, अघाए और आर्थिक रूप से सुरक्षित लोग हैं|
दसवीं दर्जे की शिक्षा है लेकिन वि.वि. और कालेजों के प्रोफेसरों की नियुक्ति करते हैं| मुश्किल से ग्रेजुएट हैं लेकिन केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के एकेडमिक कौंसिल के सदस्य हैं|
वे मेरे समकालीन हैं| वे सब महान हैं| खैर!
यहाँ गाँव में स्थितियाँ विकट हैं| पहले से भी बदतर|
ग्रामपंचायतों में इतना भ्रष्टाचार और इतनी हिंसा की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी| खदानों में नंबर दो का अवैध उत्खन हर जगह चल रहा है और इसमें समूचा राजनीतिक-प्रशासनिक तंत्र शामिल है|
मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो कहीं मुझे भी 'नक्सल' न घोषित कर दिया जाए| अगर ऐसा किया गया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने आप को वामपंथी कहने वाले सवर्ण हिन्दी लेखक, जो अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े 'लेखक संगठनों' को चलाते हैं और राजधानियों में रहते हुए अपने बेटे, दामाद, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, जाती-बिरादरी को हर सरकारी संस्थान में फिट कराते रहते हैं और जो अतीत की तमाम महा-वृत्तांतों ..१८५७, गांधी, भगत सिंह, मार्क्स-लेनिन वगैरह का नाम लेते रहते हैं, वे सब मेरी यंत्रणा में सत्ता के और मददगार होंगें|
उनके तो ऐसे बड़े-बड़े पुलिस अफसरों से करीबी रिश्ते हैं, जिनके अध्: पतन के किस्से मैं सुनता रहता हूँ| उन सबको वे मुक्तिबोध, रेणु अदि बताते रहते हैं...!ओह!
लगता है मैं इस पोस्ट को लिख नहीं पाउँगा ..! मैं अपनी उँगलियों को, जो की-बोर्ड पर चल रही हैं..अपने दिमाग से अलग नहीं कर पा रहा हूँ ..!
या हज़रत ...औलिया ...! हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे...! सच कहने की शक्ति..!
Sunday, January 16, 2011
वह, जिसे शोक कभी नहीं घेरता, वह असल में 'युगपुरुष' नामक चीज़ ही है
आज (१६ जनवरी २०११) हिंदी के वरिष्ठ कवि, आलोचक, संस्कृतिकर्मी, कला चिंतक अशोक वाजपेयी ७० वर्ष के हो रहे हैं। आज ही 'जनसत्ता' के अपने नियमित स्तंभ 'कभी-कभार' में उन्होंने लिखा है :
''किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आइये, साहित्य रचिये। यह आपका (अपना) फैसला था कि आप साहित्य और उसमें भी कविता जैसी उदास विधा में काम करेंगे। पर आप जानते हैं कि भले इस फैसले में दूसरों की कोई भूमिका नहीं थी, (लेकिन) दूसरे न होते तो आप एक अधसदी से ज्यादा इस काम में लगे न रहते, जब कि उसे छोड़ कर कुछ अधिक लाभकारी, अधिक दृश्य करने के लालच (अवसर) लगातार मिलते रहे हैं। आप अगर विरत या निराश होकर कहीं और नहीं गये तो शायद इसलिए कि आपको लगता रहा है कि दरअसल आपका असली घर भाषा है: आप उसी में रहते हैं, उसी में जीते आये हैं और उम्मीद है कि उसी में मरेंगे। यह घर ऐसा है कि वह पूरी तरह से आपने नहीं बनाया-बसाया है। उसमें दूसरों की की बड़ी भूमिका है। वे उसमें हमेशा मौज़ूद रहे हैं। भाषा एक ऐसा घर है जिसमें जब आप अकेले भी हों तो अदृश्य ढंग से ही सही, दूसरे मौज़ूद रहते हैं: शायद कवि-मित्र कमलेश ने इसी को 'खुले में आवास' कहा है और उससे भी पहले गा़लिब ने 'बेदरोदीवार का इक घर'। इस विश्वास से डिगने का कभी कभी अवसर नहीं आया कि भाषा का सच उतना ही सच है जितना कि और कई तरह के सच; कि कई मायनों में वह अधिक टिकाऊ सच है, कि वह कई बार अधिक स्मरणीय है और कि वह छोटी-छोटी सच्चाइयों को भी अपने अंदर सहेज और बचाकर रखता है।...''
.....''इसमें संदेह नहीं कि साहित्य ने अंतत: बचाया। उसने हर हालत में मनुष्य बने रह सकने का सबक कभी स्थगित नहीं किया। उसने अंधेरे को, जो हर समय बढ़ता ही जाता है, नज़रंदाज़ नहीं होने दिया, लेकिन इस उम्मीद को (भी) बनाये रखा कि अब भी रोशनी मुमकिन है; कि हम किसे न किसी रोशनी तक पहुंच सकते या उसे थोड़ी देर के लिए ही सही, पैदा कर सकते हैं..। उसने इस इच्छा को कभी शिथिल नहीं पड़ने दिया कि हमें रोशनी चाहिए और उस पर हमारा हक है।''
आप सब जो इस मेरे ब्लाग पर आते रहे हैं और अपना संबल देते रहे हैं, जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से मैं 'भाषा' को लगातार और बारबार 'शरण्य' या 'घर' कहता रहा हूं। महान भाषा-चिंतकों को भी कई बार उद्धृत करते हुए, धीमी आवाज़ में ही सही, लेकिन निरंतर कहने की कोशिश की है कि लेखक ही भाषा का मूल-निवासी या आदिवासी है और उसे वहां से बेदखल करने वाली शक्तियां वे रही हैं जो उसे अपने किसी उपनिवेश में बदलने के लिए लगातार सक्रिय रही हैं। भाषा में उसके मूल निवासी की यह ज़रा-सी जगह बची रहनी चाहिए। जब-जब ऐसा नहीं हुआ है तब-तब स्वयम लोकतंत्र की मूल प्रतिज्ञाओं का ही उल्लंघन हुआ है। आज के अपने स्तंभ 'कभी-कभार' में भी और इसके पहले भी साहित्य और कलाओं के ऐसे औपनेवेशीकरण की मुखालफ़त में, उसकी स्वायत्तता और गरिमा के पक्ष में अशोक वाजपेयी ने कई बार लिखा है। मुझे कोई कारण नहीं लगता कि उस पर अविश्वास करूं सिर्फ़ इसलिए कि इससे उनके बीच मेरी स्वीकृति बढ़ेगी, जो अर्से से उन पर अविश्वास करते रहे हैं।
यह ब्लाग मेरी निजी डायरी या निजी नोटबुक की तरह है। इसे मैं किसी साहित्यिक पत्रिका या अन्य किसी सार्वजनिक जगह की तरह नहीं बरत रहा। आज भी वही बात है। मैं खुश हूं और अशोक वाजपेयी को उनके ७० वें जन्मदिन पर ढेरों--ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और यह आकांक्षा करता हूं (शायद 'प्रार्थना' करने या 'दुआ' करने के लिए अपने दोस्तों के बीच अधिक जाना जाता हूं) कि वे इससे भी अधिक ऊर्जा और सक्रियता के साथ आने वाले सुदीर्घ समय तक वही सब कुछ करते रहें जो वे कर रहे हैं, बल्कि आधी से भी अधिक सदी से करते रहे हैं।
वे हमारे समय के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं उनका अपना एक 'आभा/ प्रभा-मंडल' है। हर बड़े ग्रह-नक्षत्र का ऐसा 'प्रभा-मंडल' होता ही है। उनके उस मंडल को बनाने वाले और उससे प्रदीप्त होने वालों में मेरी कोई जगह कत्तई नहीं है। मैं उनके विचारों और उनके विन्यासों या भाषिक भंगिमाओं का लेखक हूं भी नहीं। शायद मैं इस पल जो कुछ यहां लिख रहा हूं, वह लिखते हुए मैं लेखक भी नहीं हूं। शायद जिस स्थिति और जिस जगह पर स्वयम अशोक जी और उनके प्रभा-मंडल के अन्य लेखक हैं, वहां तक मेरे होने की टिमटिमाहट भी नहीं पहुंचती होगी। पहुंच पाती नहीं होगी। आज उनके बारे में 'जरत्कारु' और 'विष्णुप्रिया' जैसी विलक्षण कविताएं लिखने वाले, अपने भाषिक संस्कारों में मेरे भी बहुत प्रिय रहे कवि कमलेश जी ने उन पर लिखते लिखते कुछ हिचकिचाहट दिखाई है।.. मैं उस 'हिचक' को थोड़ा-सा गाढ़ी स्याही से उभारते हुए लिखना चाहता हूं कि यह स्वीकारने में अब कोई हिचक या संकोच नहीं होना चाहिए कि संस्कृति और साहित्य के निर्धारित समय और जगह में अशोक वाजपेयी निस्संदेह 'युग-पुरुष' ही हैं। उन्होंने यह 'पद' अपनी कर्मठता, प्रतिभा और संकल्प से हासिल कर डाला है। उनका यह 'युग-पौरुषत्व' कई बार दूसरों या 'अन्यों' को खटकता होगा, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है?
यह एक संयोग ही है कि कुछ साल पहले प्रख्यात आलोचक डाक्टर रामविलास शर्मा पर 'डाक्युमेंटरी' -'कालजयी मनीषा' बनाते हुए मैंने उन्हें एक जगह 'ऋषि' कह डाला था, तब बाद में यह जान कर आश्चर्य हुआ था कि लिखित में अशोक वाजपेयी यह विशेषण उन्हें कुछ पहले ही दे चुके थे। कौन नहीं जानता कि डाक्टर रामबिलास शर्मा उन विचारों के कत्तई नहीं थे, जिनके लिए अशोक जी जाने जाते हैं। सतत आमंत्रण के बावज़ूद 'भारत भवन' न आने की ज़िद और संकल्प से अविचलित रहने और तमाम तरह के प्रलोभनों के प्रति अपनी सहज विरक्ति रखने वाले, निष्कंप और खासे अकादमिक मार्क्सवादी डाक्टर रामबिलास शर्मा किसी भी तरह से अशोक वाजपेयी की सौंदर्याभिरुचि या भाषिक आस्वाद के लेखक आलोचक नहीं थे। लेकिन उनके प्रति जिस सम्मान और उदात्तता का परिचय अशोक जी ने दिया था, मुझे लगता है अभी तक 'शीतयुद्ध' की मन:स्थिति में रहे आने वाले लेखकों-आलोचकों को भी वैसे ही 'वैचारिक खुलेपन के बड़प्पन' का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अशोक वाजपेयी ने अपने कर्म और सृजन से हमारे समय में जो लंबी रेखा खींची है, उसे खरोंचने-मिटाने के प्रयत्न, मुझे पूरा विश्वास है कि अब हास्यास्पद और क्षुद्र्त्व भरे ही सिद्ध होंगे।
यह कहा जायेगा कि ऐसा 'विरुद गान' मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी-अभी 'मोहन दास' को जो साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, उसकी ज्यूरी में अशोक वाजपेयी भी थे और मैं यह उसकी कृतज्ञता के एवज में लिख रहा हूं। यहां मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अशोक जी का प्रिय कवि और रचनाकार कभी नहीं रहा (हांलाकि मेरे नये कविता-संग्रह 'एक भाषा हुआ करती है' का ब्लर्ब उन्होंने ही लिखा है) उनके स्तंभ और आलोचनात्मक लेखन में भी मेरा ज़िक्र शायद ही कहीं रहता हो। मेरी तरफ़ भी लगभग यही बात लागू होती है। मैंने उन पर कभी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा। जो भी लिखा, वह एक समय 'पोलिटकली करेक्ट' रहने के लिए, उन्हें आहत करने के लिए ही लिखा। स्वाभाविक रूप से उन्हें मेरा असंदिग्ध दुस्साध्य शत्रु होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी लगभग नहीं है। बल्कि मुझे यह बाद में पता चला कि वे साहित्य अकादमी की ज्यूरी में भी थे। यह भी बताने की कई कोशिशें हुईं कि मैं उनकी पहली पसंद नहीं था। इसे मानने में भी मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं इस तथ्य को कैसे भुलाऊं कि इसके पहले 'द्विजदेव' और 'फिर उसके बाद 'कृष्णबलदेव वैद सम्मान' के भी निर्णायक वही थे। ऐसा वे क्यों करते रहे ? मैं समझ नहीं पाता। लेकिन सच यह भी है और यह मेरा निजी सच है कि उनके लेखन और व्यक्तित्व से मै निरंतर प्रेम करता रहा हूं। मैंने अभी अपना ५८ वां साल इसी १ जनवरी को पूरा किया है, इसलिए पूरे एक युग की दूरी मेरे और उनके बीच है। वे अभी भी अपने को 'बूढ़ा' मानने से कतराते हैं, जब कि मैं बचपन से ही बूढ़ा हो चुका था। मुझे लोग बताते हैं कि जब मेरी उम्र ५-६ साल की रही होगी और लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो मैं कहा करता था 'अस्सी साल' ! ..और लोग हंसा करते थे। तो आज जब यह लिख रहा हूं तो शायद मैं दो-ढाई सौ साल का हो चुका होऊंगा...।
मैं उनकी एक कविता 'देवता हमें पुकारेंगे' की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं :
''जब पाप या प्रेम करने की बची न होगी शक्ति,
जब एक लहूलुहान भाषा और जर्जर शरीर भर होंगे पास,
जब शब्द उड़ रहे होंगे चिंदियों की तरह हवा में
तब किसी पुराने छज्जे से
स्वप्न की किसी ऊंची चट्टान से
सदियों से बंद किसी खिड़की से
देवता हमें पुकारेंगे..''
(जारी....)
(अभी तीन दिन पहले ही राजस्थान-मुंबई के सफर से लौटा हूं और अभी भी कई कामों में उलझा हुआ हूं। कल या परसों इस टिप्पणी को पूरा पोस्ट करूंगा। पिछले साल अशोक वाजपेयी का एक चित्र अपने कैमरे से खींचा था। अच्छा तो नहीं आया था, लेकिन उसे फोटोशाप से कुछ बदल कर लगा रहा हूं।)
Sunday, October 10, 2010
'पार्थक्य' और 'एकांत' और मेरी कविताएं
('पचास कविताएं' : किताब की भूमिका)
कविताएं बचपन से ही मेरे सबसे निकट रही हैं। वे मेरे अस्तित्व के एकांत, निस्संग सन्निकटता और नीरवता की सबसे भरोसेमंद और अटूट साथी रही हैं। कई बार जब यह गहरा संदेह पैदा होता है कि इस समय और स्थान में, जहां चारों ओर अनगिन सत्ताओं का सर्वव्यापी साम्राज्य है, क्या सचमुच मेरी भी कहीं कोई मौलिक सत्ता और कहीं कोई प्रामाणिक अस्तित्व है, क्या मैं भी कहीं ‘उपस्थित’ हूं, तो कविता ही उसका, कमज़ोर ही सही, पर सबसे पहला और शायद अंतिम प्रमाण होती है।
जब सारी सत्ताएं साथ छोड़ जाती हैं, या उनके फैसलों का शोर चारों ओर गूंज रहा होता है, तो वह कविता ही है, जहां अपनी आवाज़ साफ सुनाई देती है। कविता कभी भी, पराजय, विध्वंस, आत्महीनता और गहरे दुखों के पल में भी हाथ और साथ नहीं छोड़ती। वह एक ऐसे निरापद दिक-काल का निर्माण करती है, जहां पूंजी से लेकर राजनीति, धर्म, नस्ल, जाति, मास-मीडिया और तकनीक की तमाम संगठित सत्ताओं की हिंसा और अन्याय के विरुद्ध किसी वंचना या विराग में डूबा एक गरीब या फकीर अपना कोई सबसे मानवीय, नैतिक और पवित्र फैसला सुनाता है। दिक और काल, समय और यथार्थ, निजता और समूह, व्यक्ति और सत्ता-प्रणालियों के बारे में कोई धीमा, मंद, निजी निर्णय। एक ऐसा अस्फुट एकालाप, जो बहुत करीब से, ध्यान लगाकर ही सुना जा सकता है।
कविता समूची प्रकृति और मनुष्यता के उत्पीड़न और विनाश में लगी सबसे बलशाली ताकतों के ‘पाप’ (नैतिक) और ‘अपराध’ (सामाजिक-संवैधानिक) के खिलाफ़ हमेशा कोई न कोई ‘फतवा’ जारी करती रहती है और अपने जीवन को बार-बार दांव पर लगाती है। वह हर बार कोई न कोई जोखिम या खतरा मोल लेती है और हर बार किसी संयोग या चमत्कार से बच निकलने पर अपना पुनर्जीवन हासिल करती है और एक बार फिर सांस लेना शुरू करती है। फिर से किसी नये जोखिम भरे दायित्व का बोझ उठाने के लिए।
मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था और मां कैंसर में मर रहीं थीं। डाक्टरों ने जवाब दे दिया था और उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से गांव के घर में वापस ले आया गया था। पिता जी के पास सारे पैसे और जेवर खत्म हो चुके थे। अब कोई भौतिक और बाहरी मदद मां के लिए निरर्थ हो चुकी थी। वे सिर्फ अनार का रस पी रहीं थीं। तब भी वह कविता ही थी और चित्र, जिनके जरिये मैं अपनी मां को बचाने के लिए कैंसर से पूरे भरोसे के साथ लड़ रहा था। मां की मृत्यु के वर्षों बाद तक उस कमरे की दीवारों पर, जिसमें मां अपने जीवन में रहतीं थीं, मेरी बनाई अनगिनती आकृतियां थीं और उतने ही शब्द, जो उस समय मेरी समझ में अबूझ शक्तियों से भरे थे और वे मृत्यु को कहीं दूर रोक कर, मां को मेरे लिए बचा सकते थे।
ऐसा लेकिन नहीं हुआ। शब्द और दीवारों या कागज़ों पर, किसी अकेले निर्बल कलाकार या कवि द्वारा उकेरे गये अक्षर या आकार अक्सर प्रत्यक्ष और प्रबल भौतिक शक्तियों के हाथों पराजित होते हैं, मिटा दिये जाते हैं। लेकिन जिसके पास कोई और बल न हो, दूसरा कोई विकल्प ही न हो, तो बार-बार अपने इन्हीं उपकरणों की ओर लौटने के, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं होता।
तमाम सारी बाहरी ताकतें जब भाषा पर आक्रमण करती हैं और स्मृतियों का विनाश करने के अपने राजकर्म या वणिककर्म में संलग्न हो जाती हैं, तो कविता मनुष्य या किसी व्यक्ति की स्मृतियों को बचाने के प्राणपन संघर्ष में मुब्तिला होती है। विस्मरण के विरुद्ध एक पवित्र और ज़रूरी संग्राम की शुरुआत सबसे पहले कविता ही करती है, अगर वह अपने किसी अन्य हितसाधन में नहीं उलझ गयी है, और सबसे अंत तक वही उस मोर्चे पर रहती है। सबसे पहले और सबसे अंत में यह मोर्चा भाषा का ही होता है। कविता की एक ऐसी निजी कवि-भाषा, जो जीवन के अनुभवों से अपना अर्थ प्राप्त करती है, प्रचलन, प्रयोग और मुहावरों से नहीं। कविता भाषा के चालू प्रत्ययों, मुहावरों और वागाडंबरों (रेटरिक या डेमागागी) को नष्ट करती है। उन्हें प्रश्नांकित करती है। .....और जो कविता जितना अधिक यह काम करती है, वह अपने विरुद्ध उतना ही विस्मरण का विरोध एकत्र करती है।
एक तरफ वह स्मृति की रक्षा करती है, दूसरी ओर वह भाषा में शब्दों के अर्थ की भी रक्षा और उनका पुनरुद्धार करती है। वह शब्दों में नये अर्थों को आविष्कृत भी करती है। वह शब्दों को उनकी विनषट स्मृतियों के साथ बचाते हुए उन्हें किसी शरणार्थी शिविर तक पहुंचाती है। उनके घावों पर मलहम लगाती है और पट्टियां बांधती है। हमारे समय में, भाषा का अलग-अलग गैर-मानवीय या मनुष्य-विरोधी परियोजनाओं में जैसा ‘इस्तेमाल’ किया गया है, उसके संदर्भ में मुझे पोलिश भाषा के अपने प्रिय कवि ताद्युश रोज़ेविच की कविता 'शब्द’ की याद आ रही है -‘‘बचपन में शब्द मलहम की तरह घावों पर लगाये जा सकते थे/ हम दे सकते थे उसे/ जिसे हम प्यार करते थे/’’(इस कविता का अनुवाद इस ब्लाग पर पहले मैं दे चुका हूं।)
हर सच्चे कवि को संसार की बाहरी सत्ताएं भाषा और अपने समाज से हमेशा बेदखल करती हैं। वह विस्थापन और उत्पीड़न की यातना उसी तरह भोगता है जैसे कोई आदिवासी या संस्कृति और समाज का सबसे निचला वर्ग और वर्ण। वह कविता या रचना ही है, जो उसे करुणा और सहानुभूति से भरे, एक पवित्र और अपेक्षाकृत सुरक्षित शरण्य में आश्रय देती है। ......और वह थोड़ी-सी गरिमा जो हर मनुष्य और हर तरह की कला के लिए अभीष्ट है।
कहीं पढ़ा था कि कविता किसी अनजान देश के किसी छोटे-से स्टेशन के निर्जन प्लेटफार्म में देर रात खड़ी किसी रेलगाड़ी की तरह होती है। बिल्कुल खामोश। अपनी अगली यात्रा को फिलहाल कुछ समय तक स्थगित करती हुई। बीच-बीच में, कभी-कभी इंजन से निकलती भाप से ही पता चलता है कि सांस अभी कायम है। .....और अभी आगे कुछ स्टेशन और हैं, जहां तक यात्रा जारी है।
राजनीतिक सत्ताएं कभी भी किसी कविता को ईनाम नहीं देतीं। क्योंकि वे हमेशा पिछली कुछ सदियों में कविता विरोधी सिद्ध होती आई हैं। मेरा अभिप्रेत गहन मानवीय संपृक्ति और प्रतिबद्धता की कविता से है। आज तक के इतिहास में किसी भी धार्मिक या व्यापारिक या राजनीतिक सैद्धांतिकी या विचारधारा की कोई भी राज्यसत्ता ऐसी नहीं पाई गई है, जिसने प्रतिपक्ष की या किसी अकेले मनुष्य की अपने से असहमत, विसंवादी स्वर में बोलती कविता को बर्दाश्त किया हो। बेदखली, दण्ड, निर्वासन, उपेक्षा, उत्पीड़न, प्रताड़नाएं और अंतत: कवि की मृत्यु ही अक्सर ऐसी कविता का ईनाम हुआ करता है। मैं आपसे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, कि मैं ऐसा ही कवि हूं और यही बने रहना चाहता हूं।
जैसा मैंने पहले कहा, अपने बचपन से शब्दों और रंगों को मैंने अपने सबसे अधिक करीब पाया। बहुत निकट। यदि बाहर का संसार मुझे निराश और दुखी करता था, या अगर वहां रहते हुए मुझे अपने,(मुक्तिबोध के शब्दों में) ‘अकेलेपन और पार्थक्य’ का बोध होता था, या अगर वहां की सत्ताओं के सामने मैं स्वयं को बहुत निर्बल और असहायता से भरा पाता था, तो वे शब्द और रंग ही होते थे, जो मेरा संबल और मेरे सहचर बनते थे। वे बहुत नैतिक, निर्दोष, गहरी संवेदनात्मकता और सहानुभूति से भरे होते थे। मैंने उनके साथ और उन्होंने मेरे साथ बहुत-सा समय बिताया है। लगभग एक जीवन भर। इस साथ-साथ के समय का बहुत रोमांचक, कौतुक भरा, स्वप्नों और शोक-हर्ष से भरा एक अलग आख्यान है, जिसे कभी संभव हुआ तो मैं लिखूंगा। .....और आज जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, तब भी, सिर्फ वही मेरे साथ हैं। लेखक होने के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य अस्मिता नहीं है। नागरिक, पारिवारिक संबंघ-संज्ञाएं, कौटुंबिक-जातीय सूत्र, सांस्थानिक, धार्मिक-राजनीतिक संबंद्धताएं आदि जो अन्य प्रचलित-परिचित अस्मिताएं होती हैं, उनमें से अधिकांश से मुक्त होने, उन्हें छोड़ने की मैंने या तो स्वयं कोशिश की है, या फिर उनमें से बहुतेरी प्रत्यक्ष बाहरी निरंकुश और भ्रष्ट सत्ताओं द्वारा अन्यायपूर्वक मुझसे छीन भी ली गई हैं। ......और मैं एक ऐसे एकांत में घिर गया हूं, जो भाषा के तमाम सामूहिक-औपचारिक संरचनाओं और उद्यमों-व्यवसायों से बने एक शोर-ओ-गुल से भरे समाज से निर्वासन का एकांत है। यह प्रीतिकर नहीं, पीड़द है। पर यह निर्वासन इतिहास के एक बहुत विराट~ सभ्यतामूलक अनुभव के साथ भी मुझे जोड़ता है। इसीलिए यह एक ‘प्रिवेलेज’ भी है। यह एक ऐसी अवस्थिति है जो मेरे अनुभवों और अवस्थिति को, मेरी चेतना और संवेदना को इस देश की उस विराट~ वंचित मनुष्यता की नियति के साथ जोड़ देती है, विस्थापन और उत्पीड़न, संघर्ष और छलनाएं ही जिसका इतिहास है।
मुझे यह मानने में कत्तई हरबार यह दिक्कत होती है कि अपने इस ‘निर्वासन’ का निर्माण मैंने स्वयं किया है। या जैसे कि यह निर्वासन मेरी कोई अपनी चुनी हुई चीज है और अपनी इस नियति और अवस्थिति का समूचा उत्तरदायित्व मेरे अपने ऊपर ही है। ऐसा अगर कोई कहता है, तो सीधे-सीधे उस पर संदेह किया जाना चाहिए । निश्चयात्मक संदेह। क्योंकि जिस समय और यथार्थ में हम हैं, उसमें ऐसे लोग स्वयं उस सत्ता के ही प्रच्छन्न प्रतिनिधि हैं, जो इस समय के हर विस्थापित और उत्पीड़ित समूह, वर्ग, जाति या व्यक्ति की नियति का उत्तरदायी किसी उत्पीड़क सत्ता-प्रणाली को नही, बल्कि स्वयं उसी को मानते हैं, जो उसका शिकार है। वे अपराधी हैं और अलग-अलग महावृत्तांतों के मृत वागाडंबरों के पीछे छुपे अनैतिक आतताई हैं। आज के मुहावरे में वे सत्ताओं के दलाल हैं।
लेकिन यह जो निर्वासन या विस्थापन है क्या यह कोई ऐसा अलगाव है, जिसने मुझे मेरे समय और यथार्थ से काट दिया है, पृथक कर दिया है और उसकी सारी सूचनाएं मुझ तक पहुंचनी बंद हो गई हैं? मुझे लगता है वास्तविकता इसके ठीक उलट है। इस दूरी से संभवत: मुझे वह सारा प्रपंच अधिक साफ दिखाई देता है, जो निकट होने पर ओझल और अगोचर हो जाता था। मुक्तिबोध ने अपने एक निबंध में ‘एकांत’ और ‘पार्थक्य’ का महत्वपूर्ण विश्लेषण किया था -
‘‘यह पार्थक्य घनघोर है। यह मेरा किया नहीं है। मैं इस पार्थक्य का विधाता नहीं। वह मेरे ज़माने की बदनसीबी है। जिस चबूतरे पर मैं खड़ा हुआ हूं, उसके पाये का वह पाप है। आज से दस-बीस साल पहले यह कहा जाता था कि कलाकार हमेशा अकेला होता है। इस पर मेरी टिप्पणी केवल इतनी ही है कि हर आदमी को, सोचने-विचारने के लिए, मनो-मंथन के लिए, एकांत चाहिए, जिसमें केवल वह ही हो और कोई न हो। कलाकार का जीवन चूंकि अधिकतर मनोमय है (व्यस्त रहते हुए भी) इसलिए मुझे एकांत आवश्यक है। अपने मनोमय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अकेला होता है। यह स्वभाव-सिद्ध है। (लेकिन) अकेलापन और पार्थक्य में अंतर है।’
मुझे नहीं लगता कि मुक्तिबोध की तरह किसी अन्य लेखक-कवि ने अकेलेपन के ऐसे दुर्निवार एकांत का सामना कभी किया हो। निर्मल वर्मा या अज्ञेय का एकांत और अकेलापन अलग तरह का था। मुक्तिबोध के वे पत्र, जो उन्होंने अंग्रेज़ी में अपने गहरे मित्र नेमिचंद जैन को लिखे, उनके निर्वासन और पार्थक्य-बोध की सांद्र-सघन तीव्रता को सामने लाते हैं। यह अकेलापन अपनी अनुभूतिपरक बनावट में, सतह से देखने पर, पहली दृष्टि में, निर्मल वर्मा, काफ्का या किसी भी विलक्षण रचनाकार के एकांत के भले करीब लगता हो, लेकिन यह उस अप्रतिम बौद्धिक का भी अकेलापन है, जो अपने समस्त स्नायुतंत्र के साथ आत्मस्थ नहीं, मूलत: विश्वचेतस या कालचेतस है। वह तिलक की तरह जेल में रहते हुए ‘गीता-रहस्य’ भी लिख सकता है, नेहरू की तरह ‘डिस्कवरी आफ इंडिया’ भी और जूलियस फ्यूचिक की तरह ‘फांसी के फंदे से’ भी। हमारे समय के किसी भी सच्चे रचनाकार के पास असंख्य आंखें और असंख्य ‘एंटिना’, ‘राडार’ और ‘स्कैनर’ होने चाहिए। यह उसका संकटग्रस्त जीवन ही उसे दे सकता है, कोई विनिर्मित भाषिक भंगिमा नहीं। आप यातनाग्रस्त और अन्यायी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वंचित और लुटेरा दोनों कोई अगर एक साथ होने का दावा करता है, तो उसके पीछे का कोई रोचक विडंबनाओं से भरा-पूरा वृत्तांत भी ज़रूर होगा। ऐसा आज के समय में होता भी है। इसकी खोज़ मैं अक्सर कथाकार बन कर किया करता हूं और आप सब वह किस्सा तो जानते ही हैं .....।
मुक्तिबोध ने अपने इसी निबंध में एक जगह लिखा है -
‘‘किनारे रह कर, तटस्थ रह कर, (डिसएंगेज्ड रहकर, अनकमिटेड रहकर) जिंदगी जीना भद्रलोक के सफ़ेद कुर्तों के आरामकुर्सीदार वातावरण में भले ही पहुंचा दे, भले ही हम भद्रलोक की शानदार सादगी तथा आरामदेह चमकीलेपन के रंगों से अपने आसपास के अल्प-भोजियों को अपनी महत्ता का बोध करा दें, भले ही हम अपने मित-भाषण द्वारा बौद्धिक संस्कृति और कलात्मक अभिरुचि की की धाक जमा दें, किंतु हम वह ज़िंदगी नहीं जी सकते जिसे मैं, अपने शब्दों में, बिजली की तड़पदार ज़िंदगी कहता हूं। ऐसी ज़िंदगी जिसमें अछोर, भूरे, तपते मैंदानों का सुनहलापन हो, जिसमें सुलगती कल्पना छूती हुई भावना को पूरा करती है, जिसमें सीने का पसीना हो और मेहनत के बाद की आनंदपूर्ण थकन का संतोष हो। बड़ी और बहुत बड़ी ज़िंदगी जीना (इम्मेंस लिविंग) तभी हो सकता है, जब हम मानव की केंद्रीय प्रक्रियाओं के अविभाज्य और अनिवार्य अंग बन कर जियें। तभी ज़िंदगी की बिजली सीने में समाएगी।चाहे प्रगतिवादी हो या प्रयोगवादी, जिसने भी उच्च-मध्यवर्ग की सफेदपोश भद्रता के महत्व की कुर्सियों पर आराम किया कि वह गया, मर गया। ऐसा मेरा खयाल है। यह खयाल कुछ लोगों के लिए खतरनाक है-चाहे वे कितने ही प्रगतिवादी या इसके विपरीत बंगले के निवासी तकली-कातू गांधीवादी क्यों न हों! हमारे बहुत से साथी इसी ज़िंदगी में स्वर्ग देखना चाहते हैं और अपने बाल-बच्चों को स्वर्ग दिखाना चाहते हैं।’’
विख्यात पोलिश कवि, जिनका अपना जीवन भी सतत निर्वासन और यंत्रणाओं के बीच गुज़रा, अदम जगाजेयेव्स्की की कविता की पंक्तियां याद आती हैं :
'‘मैं अब पहले की तरह दर्शन शास्त्र, कविता और
दूसरी जिज्ञासाओं का छात्र नहीं रह गया हूं
मैं वह युवा कवि नहीं हूं अब
जिसने कविता की तमाम पंक्तियां लिखीं
जो भटका किया असंख्य संकरी गलियों-सड़कों
और विभ्रमों की सुरंगों में
घड़ियों की सत्ता और अंधेरे की परछाइयां ही
मेरी बरौनियां अपने हाथों से छूती थीं
लेकिन आज भी
किसी नक्षत्र का थोड़ा-सा उजाला
मुझे मेरी राह सुझाता है
और वह थोड़ा-सा उजाला ही है
जो मुझे नष्ट कर सकता है
या बचा सकता है ।''
मैं आपसे, अपने पाठकों और मित्रों और शुभेच्छुओं से बहुत भावुकता और साफगोई के साथ यह कहना चाहता हूं कि ‘वह थोड़ा-सा उजाला' मेरी कविताओं को आज तक आपसे मिला है, जिसने मुझे हमेशा नष्ट होने से बचाया है। शायद यही कारण है कि मेरे दो-तीन दशक पूर्व प्रकाशित कविता संग्रहों से लेकर हाल-फिलहाल के संग्रह तक, अपने नये-नये संस्करणों में लगातार आते रहे, भले ही मैं आलोचकों-आचार्यों की कवि-कुल- सांस्थानिक सूचियों में अनुपस्थित पाया जाऊं। यह सब आप सबके कारण ही संभव हुआ। यह सच है। मैं बहुत सहज होकर, समूची विनम्रता के साथ यह सच भी कह रहा हूं कि मैंने कवि होने के लिए कोई अन्य उपक्रम कभी नहीं किये।
आप सबके प्रति गहरी कृतज्ञता से भरा मैं अपने अलग-अलग संग्रहों की पिछली पचास कविताओं के साथ इस किताब में एक जगह उपस्थित हूं।
वैशाली, सोमवार, 4 अक्तूबर, 2010
(‘भारत भूषण अग्रवाल सम्मान’ की 25 वीं वर्षगांठ के समय इसका किंचित- तात्कालिक और संक्षिप्त रूप लिखा गया था। प्रस्तुत संकलन की भूमिका के लिए मैंने उसे अधिक परिवर्धित और कुछ विस्तृत किया है। यह किताब वाणी प्रकाशन से शीघ्र प्रकाशित हो रही है।)
Monday, September 20, 2010
'तिरिछ' : वे चार पत्र जो किस्सा बन गये
कल रात पुरानी चिट्ठियों की फाइल उलटते-पलटते कुछ ऐसे भी पत्र मिले जो अब, इतने वर्षों बाद, स्मृतियों में किसी कहानी की तरह ही कौंधते हैं। आप सब, जो मेरे लिखे को पसंद करते हैं, के अलावा ये पत्र भी ऐसे हैं, जो लिखते रहे आने का ढाढ्स और भरोसा देते हैं।
ये तीनों पत्र आज से लगभग चौथाई सदी पहले (२५ साल के आसपास) लिखी गयी कहानी 'तिरिछ' से संबंधित हैं। इनमें से एक पत्र तो मेरे दोस्त और साथी सफ़दर हाश्मी का है और अन्य तीन पत्रों में से दो इसी कहानी की एक पाठिका पूनम वर्मा के पत्र हैं। उनके कुल चार पत्र मुझे मिले थे, जिनमें से एक तो मेरे जन्मदिन की बधाई (१ जनवरी) का कार्ड था, दूसरा कहीं खो गया। उस खोये हुए पत्र की कुछ यादें अभी भी बाकी हैं। तीसरा पत्र एक अप्रत्याशित-सा पत्र था।
कई बार लगने लगता है, किसी लेखक का जीवन, समय के साथ-साथ बीतते हुए, किसी किस्से जैसा ही होता जाता है।
इसे अपने ब्लाग में इसलिए भी प्रस्तुत कर रहा हूं कि किसी भी रचना की गरिमा, उसके अर्थ और महत्व का असली आधार उसके पाठकों की स्वीकृति और उनकी प्रतिकृया ही होती है। ऐसे लेखक, जो अपनी भाषा में कुछ नया और प्रचलन से हटकर कुछ करने का जोखिम उठाते हैं, उन्हें शक्ति, प्रेरणा और संबल हमेशा अपने पाठकों से ही मिलता है। सांस्थानिक और जिसे 'मुख्यधारा' की आलोचना के नाम से जाना जाता है, वह प्रचलित और वर्चस्वशील आलोचना अपनी ताकत भर इसे अस्वीकृत करती है।

।
ये तीनों पत्र आज से लगभग चौथाई सदी पहले (२५ साल के आसपास) लिखी गयी कहानी 'तिरिछ' से संबंधित हैं। इनमें से एक पत्र तो मेरे दोस्त और साथी सफ़दर हाश्मी का है और अन्य तीन पत्रों में से दो इसी कहानी की एक पाठिका पूनम वर्मा के पत्र हैं। उनके कुल चार पत्र मुझे मिले थे, जिनमें से एक तो मेरे जन्मदिन की बधाई (१ जनवरी) का कार्ड था, दूसरा कहीं खो गया। उस खोये हुए पत्र की कुछ यादें अभी भी बाकी हैं। तीसरा पत्र एक अप्रत्याशित-सा पत्र था।

कई बार लगने लगता है, किसी लेखक का जीवन, समय के साथ-साथ बीतते हुए, किसी किस्से जैसा ही होता जाता है।
इसे अपने ब्लाग में इसलिए भी प्रस्तुत कर रहा हूं कि किसी भी रचना की गरिमा, उसके अर्थ और महत्व का असली आधार उसके पाठकों की स्वीकृति और उनकी प्रतिकृया ही होती है। ऐसे लेखक, जो अपनी भाषा में कुछ नया और प्रचलन से हटकर कुछ करने का जोखिम उठाते हैं, उन्हें शक्ति, प्रेरणा और संबल हमेशा अपने पाठकों से ही मिलता है। सांस्थानिक और जिसे 'मुख्यधारा' की आलोचना के नाम से जाना जाता है, वह प्रचलित और वर्चस्वशील आलोचना अपनी ताकत भर इसे अस्वीकृत करती है।

।
इन पत्रों को मैं अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के लिए ही यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि सच यही है कि वही मेरे शब्दों को शक्ति और उन पर मुझे भरोसा देते हैं। इन पत्रों पर या इन्हें यहां प्रस्तुत करने पर लेखकों की बहस वगैरह से मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। एक फ़िल्म कभी देखी थी, उसका एक पात्र अदालत में न्यायाधीश से यह प्रश्न पूछता है: 'ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जो भी व्यक्ति अपने देश के लोगों से प्यार करता है, और लोग भी जिसे अपना लेते हैं, उस देश की 'सरकार' (गवर्नमेंट) या सत्ताएं उसकी शत्रु हो जाती है?'
(इस पोस्ट को ब्लाग में लगाने के कुछ ही देर बाद कुछ मित्रों ने कहा कि अब तो ऐसे पत्र ही लिखे जाने बंद हो गये हैं। ईमेल और एस.एम.एस. का ज़माना आ गया है। संयोग ही था कि तीन साल पहले इसी कहानी के कन्नड़ अनुवाद पर 'संस्कार' जैसे कालजयी उपन्यास के रचनाकार, सुविख्यात महान साहित्यकार यू.आर.अनंतमूर्ति जी का एक' ईमेल' भी मुझे मिला था, जो बाद में किसी पत्रिका में छपा था, उसे भी पोस्ट कर रहा हूं। )
Friday, September 10, 2010
मेधा पाटकर की कविता की 'अंतर' और 'उत्तर-पाठिकता' : एक विचार
(१९९६ में बरगी बांध के विस्थापितों के लिए किए जा रहे आंदोलन में भाग लेते हुए मेधा पाटकर को वहां के कलेक्टर और एस.पी. ने रुखन जंगल के वन विभाग के रेस्ट हाउस में १३ दिन तक रखा था। इसी में एक तेंदुआ भी पिंजड़े में रखा गया था। कहा जा सकता है कि सरकारी रेस्ट हाउस, जो सिर्फ़ सरकारी अफ़सरों और राजनीतिक नेताओं आदि (तथा उनका खुशामदी, उन पर आश्रित वह वर्ग जिसे हम चोम्सकी जैसे चिंतकों के शब्दों में 'अदृश्य सरकार' (इनविजिबिल गवर्नमेंट) कहते हैं ) के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, उसमें मेधा पाटकर और वह तेंदुआ, दोनों कैद में ही थे। मेधा पाटकर ने यह कविता उन्हीं दिनों लिखी थी। पहली बार यह कोलकता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका- 'वागर्थ' के सितंबर, २०१० अंक में प्रकाशित हुई है। यह कविता आप भी पढें। लेकिन इस कविता को पढ़ते हुए इसके 'अंतर-पाठ' और 'उत्तर-पाठ' पर ज़रूर विचार करें, यह मेरा आग्रह है। निहायत सहज भाषा में, अत्यंत साधारण सी लगती इस कविता का 'अंतर-पाठ' हमारे आज के समय के गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक संकेतों को अंतर्भूत करता चलता है। इस कविता में आने वाले - 'छंद-मुक्त तेंदुआ और मैं' , 'रक्षा-बंधन में आज/ कल और इस पल भी/ तेंदुआ और मैं..' , 'व्यवस्था के कब्ज़े में अस्त-व्यस्त/ तेंदुआ और मैं/' , बंदूकों की नलियों में ठुसे अंधेरों में/ निद्रित तेंदुआ और मैं/' 'रेस्ट हाउस में एवरेस्ट के पहरेदार / तेंदुआ और मैं..' जैसी सरल और समकालीन हिंदी कविता में प्रचलित भाषिक संरचनाओं में लगभग अनुपयु्क्त या विसंवादी-सी लगती अभिव्यक्तियां वस्तुत: ऐसी अर्थवान कूट-संरचनाएं हैं; जिनके अर्थ कविता, लोकतंत्र, स्त्री अस्मिता, पितृसत्तात्मकता, राजनीतिक -प्रणाली, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों की वास्तविक अवस्थितियों की पहचान तक पहुंच कर खुलते हैं या 'डिकोड' होते हैं।
हमारा आज का साहित्य जिन 'जगहों' से संचालित और सम्मानित-प्रतिष्ठित होता है, कविता का 'उत्तर-पाठ' उस 'पद-कूट' को रोज़-रोज़ इस्तेमाल से घिसे हुए 'रेस्ट हाउस' जैसे मामूली संबोधन से अचानक एक ऐसे गहरे और चिंताजनक अर्थाशय से संपृक्त कर देता है, कि यह कविता मामूली नहीं रह जाती, आज के समय के गहरे संकटों और उत्पीड़न के कई 'रूपों' को निर्भयता से खोलने वाली एक महत्वपूर्ण कविता बन जाती है।
यह असंदिग्ध रूप से किसी भी भारतीय भाषा की ही एक 'समकालीन' कविता है, क्योंकि 'मराठी' या 'हिंदी' जैसा साधारण लगने वाला, एक किसी 'भाषा' को संकेतित करने वाला शब्द भी, 'एक वचन' नहीं। अपने कथ्य में हमारे देश में आज के सबसे गंभीर संकट और विडंबना को धारण करने के कारण यह 'विश्व-कविता' का सहज हिस्सा बन सकने की संभावना और सामर्थ्य रखती है। इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए।
पर्यावरण और नागरिक-मानवीय अधिकारों के लिए वर्षों से इस संघर्षरत शांतिकामी महान व्यक्तित्व की यह कविता प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व और सार्थकता की अनुभूति, दोनों एक साथ है। आशा है आप भी इसे पढ़ेंगे। )
रेस्ट हाउस, तेंदुआ और मैं
मेधा पाटकर
निर्जन वन के आवरण में 'सुरक्षित'
तेंदुआ और मैं
हरे भरे बादलों और सूरज की धार से
छंद मुक्त तेंदुआ और मैं
बंदूकों की नलियों में ठुंसे अंधेरे में
निद्रित तेंदुआ और मैं
हर सुबह की आहट से दूर
तेंदुआ और मैं
रक्षा-बंधन में आज
कल और इस पल भी
तेंदुआ और मैं
अपनी ही आवाज़ सुनने में व्यस्त
तेंदुआ और मैं
बाहर से भीतर-निडर
तेंदुआ और मैं
व्यवस्था के कब्ज़े में अस्त-व्यस्त
तेंदुआ और मैं
रेस्ट हाउस में एवरेस्ट के पहरेदार
तेंदुआ और मैं।
(अनु. परवीन जहांगीर, इस कविता को उपलब्ध कराने में सिवनी निवासी व्रजकिशोर चौरसिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे बरगी बांध आंदोलन में मेधा जी के साथ रहे हैं। अगर उन्होंने इस कविता को सुरक्षित न रख लिया होता, तो यह 'वागर्थ ' के माध्यम से हम तक न पहुंच पाती)
हमारा आज का साहित्य जिन 'जगहों' से संचालित और सम्मानित-प्रतिष्ठित होता है, कविता का 'उत्तर-पाठ' उस 'पद-कूट' को रोज़-रोज़ इस्तेमाल से घिसे हुए 'रेस्ट हाउस' जैसे मामूली संबोधन से अचानक एक ऐसे गहरे और चिंताजनक अर्थाशय से संपृक्त कर देता है, कि यह कविता मामूली नहीं रह जाती, आज के समय के गहरे संकटों और उत्पीड़न के कई 'रूपों' को निर्भयता से खोलने वाली एक महत्वपूर्ण कविता बन जाती है।
यह असंदिग्ध रूप से किसी भी भारतीय भाषा की ही एक 'समकालीन' कविता है, क्योंकि 'मराठी' या 'हिंदी' जैसा साधारण लगने वाला, एक किसी 'भाषा' को संकेतित करने वाला शब्द भी, 'एक वचन' नहीं। अपने कथ्य में हमारे देश में आज के सबसे गंभीर संकट और विडंबना को धारण करने के कारण यह 'विश्व-कविता' का सहज हिस्सा बन सकने की संभावना और सामर्थ्य रखती है। इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए।
पर्यावरण और नागरिक-मानवीय अधिकारों के लिए वर्षों से इस संघर्षरत शांतिकामी महान व्यक्तित्व की यह कविता प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व और सार्थकता की अनुभूति, दोनों एक साथ है। आशा है आप भी इसे पढ़ेंगे। )
रेस्ट हाउस, तेंदुआ और मैं
मेधा पाटकर
निर्जन वन के आवरण में 'सुरक्षित'
तेंदुआ और मैं
हरे भरे बादलों और सूरज की धार से
छंद मुक्त तेंदुआ और मैं
बंदूकों की नलियों में ठुंसे अंधेरे में
निद्रित तेंदुआ और मैं
हर सुबह की आहट से दूर
तेंदुआ और मैं
रक्षा-बंधन में आज
कल और इस पल भी
तेंदुआ और मैं
अपनी ही आवाज़ सुनने में व्यस्त
तेंदुआ और मैं
बाहर से भीतर-निडर
तेंदुआ और मैं
व्यवस्था के कब्ज़े में अस्त-व्यस्त
तेंदुआ और मैं
रेस्ट हाउस में एवरेस्ट के पहरेदार
तेंदुआ और मैं।
(अनु. परवीन जहांगीर, इस कविता को उपलब्ध कराने में सिवनी निवासी व्रजकिशोर चौरसिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे बरगी बांध आंदोलन में मेधा जी के साथ रहे हैं। अगर उन्होंने इस कविता को सुरक्षित न रख लिया होता, तो यह 'वागर्थ ' के माध्यम से हम तक न पहुंच पाती)
Friday, August 27, 2010
पाठ से पहले एक पूर्व-पीठिका (दो)
बहुत पहले, आकाशवाणी से प्रसारित रघुवीर सहाय द्वारा लिए गये एक लंबे साक्षात्कार में अज्ञेय ने रचना और रचनाकार के बीच के इस अंतराल या अलगाव को बहुत संलग्नता और गंभीरता के साथ विश्लेषित किया था। इसके लिए उन्होंने टी.एस. इलिएट के निबंधों और कविता-आलोचना की पुस्तक ‘दि सैक्रेड वुड’ का संदर्भ दिया था। इलिएट की इस पुस्तक से स्वयं उनकी अपनी आलोचना बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित थी, यह उन्होंने इस साक्षात्कार में स्वीकार भी किया था।
संभवतः उस बातचीत के समय, इसी पुस्तक में संकलित इलिएट का बहुपठित निबंध ‘पंरंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा’ उनकी स्मृति में रहा होगा। इस निबंध में इलिएट ने लिखा है कि ‘मृत लेखक हमें अपने से बहुत दूर इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी रचनाओं के जरिये हम उन्हें (बाद में) ज़्यादा नज़दीकी से जान चुके होते हैं।’ उसके अनुसार ‘कलाकार (या लेखक) का कर्म या प्रगति उसका निरंतर आत्मबलिदान और अपने व्यक्तित्व का निरंतर विलोपन (Extinction) या संहार है।’
यानी लेखक नही, उसकी रचनाओं के पाठ ही उसकी निकट अस्मिता या पहचान के शेष सबूत या साक्ष्य होते हैं, स्वयं लेखक और उसका निजी जीवन नहीं।
विलक्षण कला-चिंतक वाल्टर बेंजमिन का भी कथाकार के बारे में मत था-‘भले ही कथाकार का नाम हमारे लिए परिचित हो, लेकिन अपने जीवन की सन्निकटता में वह किसी भी अर्थ में एक समकालिक शक्ति नहीं होता। वह तो हमसे दूर हो चुका कोई व्यक्तित्व है, जो हर पल हमसे और अधिक दूर होता जाता है।’
दुर्भाग्य से हिंदी के हर आलोचक के पास उसकी राजनीति, धर्म, संघ-संगठन या क्षेत्रीय-जातीय हितों से जुड़ा प्लेटो जैसा कोई न कोई ‘रिपब्लिक’ पहले से रहता है, जिसमें से वह ‘विधर्मी-विजातीय’ कवि को बलात् निर्वासित कर देना चाहता है। इसके लिए वह कोई भी औज़ार चुन सकता है। ऐसा आलोचक पाठ के विरुद्ध दरअसल एक अघोषित ‘युद्ध’ छेडता है, और युद्ध में तो वैसे ही ‘सब कुछ जायज’ माना जाता है। उसके पास यथार्थ की कोई न कोई बनी-बनाई अवधारणा पहले से रहती है और भले ही बदले हुए दिक और काल द्वारा निरस्त किया जा चुका एक ऐसा पूर्वग्रह भी, जिसे वह ‘विचारधारा’ या किसी दूसरी सैद्धांतिकी के नाम की छद्म वैधता देते हुए, उससे रचना के पाठ का ‘विश्लेषण’(?) करता है।
बस ठीक यही वह बिंदु है जहां से समस्या, संकट, संदेह और सवाल जन्म लेते हैं। क्या वह आलोचक, उसकी आलोचना और उसकी प्रणाली सचमुच पाठ के ‘विश्लेषण या व्याख्या के लिए उपयुक्त और वैध है? और क्या वह पाठ के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वह सचमुच ‘व्याख्या’ ही है? या कुछ और ?
कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि एक विख्यात आलोचक ने कहा था, कि आलोचक का यह कार्य वर्चस्वशील सांस्कृतिक-राजनीतिक सत्ता के औज़ारों-उपकरणों द्वारा रचना के ‘पाठ’ का उत्पीड़न और उस पर विजातीय आक्रमण है। पाठ की जबरिया खुदाई, बलात् उत्खनन। पाठ में सहज रूप से उपस्थित मूल अर्थों-अभिप्रेतों का वैसा ही विस्थापन, जैसा किसी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों या मूल निवासियों का उनकी नैसर्गिक ‘मातृ-भूमि’ से होता है।
पाठ के साथ यह व्यवहार आलोचना जिन प्रचलित-चालू पारिभाषिक पदों और पद्धतियों के ज़रिये करती है, अगर आप उन्हें चिन्हित और प्रश्नांकित करें, उन पर संदेह करें, तो उसके द्वारा की गई सारी व्याख्या अपनी आलोचना के साथ धराशायी हो जाती है।
प्रख्यात आलोचक सुज़ान सोंटाग, जिनका हवाला मैं पहले भी देता रहा हूं, ने कहा है - ‘व्याख्या या आलोचना स्वयम् में कोई चरम मूल्य नहीं है, कोई ऐसा पवित्र-तटस्थ बौद्धिक कर्म, जिसकी उपस्थिति किसी ऐसी क्षमता के भीतर है, जो कालातीत हो। वह (आलोचना) स्वयम् संदिग्ध है। अब ज़रूरत स्वयं व्याख्या की व्याख्या और मनुष्य की चेतना के ऐतिहासिक परिसंदर्भ में आलोचना के मूल्यांकन और पड़ताल की है। कुछ भाषाओं-संस्कृतियों में आलोचना अपने समाज के मृत और जड़ हो चुके अतीत को बदलने, संशोधित करने और उसका पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयत्न करती है, या उससे मुक्ति के लिए संघर्ष करती है लेकिन कुछ भाषा-संस्कृतियों में यह पुरातनतावादी, कायर, भोंथरी और दमनकारी होती है।’
हिंदी में यही दूसरी स्थिति है। वह अधिकांश रचनाकारों और पाठकों के सम्मुख आज की राजनीति (जिसका वह स्वयम् आवयविक विस्तार और अनुषग है) की ही तरह अपनी वैधता और विश्वसनीयता खो चुकी है, उसके मुखौटे उतर चुके हैं, वह बेपर्दा हो चुकी है। लेकिन शायद अभी तक उसे या तो इसका बोध नहीं है, या फिर सत्तांध हो कर वह फाशीवादी विचार के जनक कहे जाने वाले दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की इस उक्ति पर अभी भी विश्वास रखती है कि ‘सत्य अपने आप में कुछ और नहीं होता, सत्य की व्याख्याएं ही सत्य हुआ करती हैं।’ या गोएबेल्स की वह कुख्यात उक्ति कि ‘झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे।’ इसका अमल हिंदी की फ़र्ज़ीआलोचना ने खूब किया है। (विडंबना बस यही है कि इसका सबसे अधिक लाभ स्वयं को परिवर्तनकामी और अग्रगामी कहने वाले कवियों-लेखकों ने उठाया है।)
इन दिनों सर्वत्र दिखाई देती आलोचना की दबंगई, अहंकार, निर्लज्जता और उसकी सनक के पीछे शायद यही धारणा काम कर रही है। वह कभी मनमाने और कभी किसी सोची-विचारी साजिश के तहत किसी रचना के ‘पाठ’ के पक्ष या विपक्ष में ऐसी आधारहीन, अनैतिक और अननुपातिक (हाइपरट्रॉफिकल) (दुः)‘व्याख्या’ को अंजाम देती है, जिससे किसी उत्कृष्ट रचना का अर्थ और महत्व नष्ट हो तथा उसके स्थान पर उसके अभीप्सित, उसके गुट के किसी ओछे या निम्नतर पाठ (और इसकी आड़ में उसके लेखक) को प्रतिस्थापित किया जा सके।
खुद सोचिये, एक एक ऐसे जटिल और बहुजन-समाज की संस्कृति, जिसकी सबसे बड़ी विडंबना उसकी लगातार बढ़ती अतिसंवेदी असहिष्णुता, अतिरेकी, हिंस्र और अराजक होती मानसिकता और प्रतिहिंसात्मक वृति है, उसमें आलोचक की यह अतिरंजित निहद्द ‘हाइपरट्रॉफी’, उसका फुफकारता-फुंसेटता, फेंचकुर फेंकता उद्दंड प्रलाप क्या विकल-उन्मादी मस्तिष्क का किसी निहत्थी रचना और उसके पाठ पर लंपट ‘हमला’ नहीं ? ....और उसके द्वारा की जाने वाली ‘व्याख्या’ क्या वही नहीं है, जिसकी शिनाख़्त सुजा़न सोंटाग ने इन शब्दों में की थी -‘ऐसी व्याख्या अतिरेकी बुद्धि द्वारा, रचनात्मक ऊर्जा और ऐंद्रिक संवेदनशीलता की कीमत पर, कला के साथ की गई एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है।’
मैं अपनी कहानियों के इस संचयन के पहले ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी कहानियों के ‘पाठ’ के साथ ही नहीं, स्वयं मेरे निजी जीवन के साथ भी हिंदी की प्राध्यापकीय या सत्ताकेंद्रित आलोचना तथा उनसे अनिवार्य रूप से संबंद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थानों ने यही ‘प्रतिशोधात्मक कार्रवाई’ पिछले कई दशकों से, बार-बार की है। इसके द्वारा उसने रचना के पाठ और उसके अर्थाशयों को क्षतिग्रस्त तो किया ही है, एक नागरिक लेखक के बतौर उसने इन कहानियों के लेखक को एक गरिमाहीन, सामाजिक-आर्थिक अनिश्चयात्मकताओं से भरे निर्वासन की ओर धकेलने की लगातार कोशिश की है। इसमें वह एक हद तक कामयाब इस मायने में रही है कि उसने इस जीवन की वास्तविक सूचनाओं को अपनी सामूहिक-सांगठनिक ताकत के ज़रिये या तो सेंसर किया है या उन्हें अफवाहों से विस्थापित किया है। मेरी ही एक कविता की पंक्ति है-‘जो यथार्थ को व्यक्त करता है, वह मार दिया जाता है अफवाहों से।’
अगर आप मेरी कहानियों-कविताओं और उनसे संबंधित हिंदी की आलोचना आदि से परिचित हैं तो ‘टेपचू’ और ‘तिरिछ’ जैसी प्रारंभिक कहानियों से लेकर ‘वारेन हेंटिंग्स का सांड’, ‘पॉल गोमरा का स्कूटर’, ‘और अंत में प्रार्थना’ जैसी बीच की, और ‘पीली छतरी वाली लड़की’, ‘मोहन दास’ और ‘दिल्ली की दीवार’ या ‘मैंगोसिल’ जैसी हाल-फिलहाल की कहानियों-लघु-उपन्यासों को लेकर हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में आलोचकों-संपादकों द्वारा चलाये गये ‘विवादों’ से भी परिचित होंगे। उन विवादों के स्तर और उनके ‘मकसद’ को लेकर, या उनके पीछे उपस्थित सत्ता-केंद्रों के बारे में मैं अलग से कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यहां मुझे अपने प्रिय और अत्यंत प्रतिभाशाली आलोचक वाल्टर बेंजमिन की फिर याद आती है, जिन्होंने ‘कहानीकार’ शीर्षक से अपने प्रिय कथाकार निकोलोइ लेस्कोव (The Storyteller:Reflections on the works of Nikoloi Leskov) के बहाने किसी किस्सागो की रचना और उसके जीवन में आने वाले संकटों-चुनौतियों का गंभीर और अविस्मरणीय विश्लेषण किया था।
बीसवीं सदी में, प्रथम विश्युवद्ध की हिंसा और अमानवीय विभीषिका में से होकर और बचकर जो लेखक लौटा था, उसके आत्मानुभव इतने आक्रांत करने वाले थे कि वह स्वयं को लंबे समय तक ‘निर्वाक्’ पाता रहा। उसके भीतर यह आशंका निरंतर थी कि वे ताकतें जो उस हिंसा और संहार में सम्मिलित थीं, वे प्रच्छन्न रूप से संस्कृति और समाज में, हार या जीत से अलहदा, ज्यों की त्यों मौज़ूद हैं।
आप स्वयं सोचिये बेंजामिन यह तब लिख रहे थे, जब यूरोप में नाजीवाद मानवता को दूसरे विश्वयुद्ध की ओर धकेल रहा था। वहां का नस्लवाद, जो किसी भी मायने में हमारे देश के जातिवाद और सांप्रदायिकता से कमतर नहीं है, बीसवीं सदी के मध्य में जिस भय और आतंक को रच रहा था, उसमें बेंजमिन जैसे अत्यंत संवेदनशील कला-चिंतक की पहली चिंता यही थी कि ‘क्या अब कोई कथाकार कहानी में सच लिखने का साहस दिखा पाएगा? क्या कहानी अपने अंत के कगार तक पहुंच गई है? हमें अब (अपने समय की) कहानी कहने वाले कथाकार कम से कम क्यों दिखते हैं? वह जो अब से कुछ समय पहले तक हमसे अविच्छिन्न था, उसे हमसे अचानक किसने छीन लिया है?’
जब मैं अपनी कहानियों और जीवन के बारे में सोचता हूं, तो वाल्टर बेंजमिन का निबंध अक्सर याद आता है।
मुझे खुशी यही है कि पाठकों ने, जिनमें हिंदी ही नहीं अन्य भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के पाठक बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं, मेरी रचनाओं को अपनाया। अन्य भाषाओं के विद्वानों और वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त आलोचकों-विचारकों ने भी इन रचनाओं को महत्व और अपूर्व सम्मान दिया। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जिन रचनाओं के कारण हिंदी सत्ता-केंद्रों और प्रतिष्ठानों ने, जातीय तथा राजनीतिक पूर्वग्रहों के चलते, मुझे प्रताड़ना, लांछनाएं और कष्टप्रद ओछे विवाद दिये, उन्हीं रचनाओं के अन्य भाषाओं में अनुवादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिली।
मैंने इस संग्रह में जान-बूझ कर उन कहानियों को भी सम्मिलित किया है, जिनकी ‘व्याख्याएं’ अनेक रूपों में हिंदी की प्रचलित आलोचना में आपको यहां-वहां मिलेंगी। अब इस संकलन के माध्यम से आपके पास उन कहानियों का मूल ‘पाठ’ है, आप स्वयं इस पर अपना मत देंगे।
कहानी एक ऐसी जनप्रिय कला है, जिस पर समय-समय की तमाम सत्ताओं द्वारा लगाए गये अभियोगों पर अंतिम फैसला, पाठकों की ‘जन-अदालत’ ही देती है।
तो आपके कठघरे में अपनी दस प्रिय कहानियों को खड़ा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है आप इस चयन को पसंद करेंगे।
संभवतः उस बातचीत के समय, इसी पुस्तक में संकलित इलिएट का बहुपठित निबंध ‘पंरंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा’ उनकी स्मृति में रहा होगा। इस निबंध में इलिएट ने लिखा है कि ‘मृत लेखक हमें अपने से बहुत दूर इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी रचनाओं के जरिये हम उन्हें (बाद में) ज़्यादा नज़दीकी से जान चुके होते हैं।’ उसके अनुसार ‘कलाकार (या लेखक) का कर्म या प्रगति उसका निरंतर आत्मबलिदान और अपने व्यक्तित्व का निरंतर विलोपन (Extinction) या संहार है।’
यानी लेखक नही, उसकी रचनाओं के पाठ ही उसकी निकट अस्मिता या पहचान के शेष सबूत या साक्ष्य होते हैं, स्वयं लेखक और उसका निजी जीवन नहीं।
विलक्षण कला-चिंतक वाल्टर बेंजमिन का भी कथाकार के बारे में मत था-‘भले ही कथाकार का नाम हमारे लिए परिचित हो, लेकिन अपने जीवन की सन्निकटता में वह किसी भी अर्थ में एक समकालिक शक्ति नहीं होता। वह तो हमसे दूर हो चुका कोई व्यक्तित्व है, जो हर पल हमसे और अधिक दूर होता जाता है।’
दुर्भाग्य से हिंदी के हर आलोचक के पास उसकी राजनीति, धर्म, संघ-संगठन या क्षेत्रीय-जातीय हितों से जुड़ा प्लेटो जैसा कोई न कोई ‘रिपब्लिक’ पहले से रहता है, जिसमें से वह ‘विधर्मी-विजातीय’ कवि को बलात् निर्वासित कर देना चाहता है। इसके लिए वह कोई भी औज़ार चुन सकता है। ऐसा आलोचक पाठ के विरुद्ध दरअसल एक अघोषित ‘युद्ध’ छेडता है, और युद्ध में तो वैसे ही ‘सब कुछ जायज’ माना जाता है। उसके पास यथार्थ की कोई न कोई बनी-बनाई अवधारणा पहले से रहती है और भले ही बदले हुए दिक और काल द्वारा निरस्त किया जा चुका एक ऐसा पूर्वग्रह भी, जिसे वह ‘विचारधारा’ या किसी दूसरी सैद्धांतिकी के नाम की छद्म वैधता देते हुए, उससे रचना के पाठ का ‘विश्लेषण’(?) करता है।
बस ठीक यही वह बिंदु है जहां से समस्या, संकट, संदेह और सवाल जन्म लेते हैं। क्या वह आलोचक, उसकी आलोचना और उसकी प्रणाली सचमुच पाठ के ‘विश्लेषण या व्याख्या के लिए उपयुक्त और वैध है? और क्या वह पाठ के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वह सचमुच ‘व्याख्या’ ही है? या कुछ और ?
कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि एक विख्यात आलोचक ने कहा था, कि आलोचक का यह कार्य वर्चस्वशील सांस्कृतिक-राजनीतिक सत्ता के औज़ारों-उपकरणों द्वारा रचना के ‘पाठ’ का उत्पीड़न और उस पर विजातीय आक्रमण है। पाठ की जबरिया खुदाई, बलात् उत्खनन। पाठ में सहज रूप से उपस्थित मूल अर्थों-अभिप्रेतों का वैसा ही विस्थापन, जैसा किसी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों या मूल निवासियों का उनकी नैसर्गिक ‘मातृ-भूमि’ से होता है।
पाठ के साथ यह व्यवहार आलोचना जिन प्रचलित-चालू पारिभाषिक पदों और पद्धतियों के ज़रिये करती है, अगर आप उन्हें चिन्हित और प्रश्नांकित करें, उन पर संदेह करें, तो उसके द्वारा की गई सारी व्याख्या अपनी आलोचना के साथ धराशायी हो जाती है।
प्रख्यात आलोचक सुज़ान सोंटाग, जिनका हवाला मैं पहले भी देता रहा हूं, ने कहा है - ‘व्याख्या या आलोचना स्वयम् में कोई चरम मूल्य नहीं है, कोई ऐसा पवित्र-तटस्थ बौद्धिक कर्म, जिसकी उपस्थिति किसी ऐसी क्षमता के भीतर है, जो कालातीत हो। वह (आलोचना) स्वयम् संदिग्ध है। अब ज़रूरत स्वयं व्याख्या की व्याख्या और मनुष्य की चेतना के ऐतिहासिक परिसंदर्भ में आलोचना के मूल्यांकन और पड़ताल की है। कुछ भाषाओं-संस्कृतियों में आलोचना अपने समाज के मृत और जड़ हो चुके अतीत को बदलने, संशोधित करने और उसका पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयत्न करती है, या उससे मुक्ति के लिए संघर्ष करती है लेकिन कुछ भाषा-संस्कृतियों में यह पुरातनतावादी, कायर, भोंथरी और दमनकारी होती है।’
हिंदी में यही दूसरी स्थिति है। वह अधिकांश रचनाकारों और पाठकों के सम्मुख आज की राजनीति (जिसका वह स्वयम् आवयविक विस्तार और अनुषग है) की ही तरह अपनी वैधता और विश्वसनीयता खो चुकी है, उसके मुखौटे उतर चुके हैं, वह बेपर्दा हो चुकी है। लेकिन शायद अभी तक उसे या तो इसका बोध नहीं है, या फिर सत्तांध हो कर वह फाशीवादी विचार के जनक कहे जाने वाले दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की इस उक्ति पर अभी भी विश्वास रखती है कि ‘सत्य अपने आप में कुछ और नहीं होता, सत्य की व्याख्याएं ही सत्य हुआ करती हैं।’ या गोएबेल्स की वह कुख्यात उक्ति कि ‘झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे।’ इसका अमल हिंदी की फ़र्ज़ीआलोचना ने खूब किया है। (विडंबना बस यही है कि इसका सबसे अधिक लाभ स्वयं को परिवर्तनकामी और अग्रगामी कहने वाले कवियों-लेखकों ने उठाया है।)
इन दिनों सर्वत्र दिखाई देती आलोचना की दबंगई, अहंकार, निर्लज्जता और उसकी सनक के पीछे शायद यही धारणा काम कर रही है। वह कभी मनमाने और कभी किसी सोची-विचारी साजिश के तहत किसी रचना के ‘पाठ’ के पक्ष या विपक्ष में ऐसी आधारहीन, अनैतिक और अननुपातिक (हाइपरट्रॉफिकल) (दुः)‘व्याख्या’ को अंजाम देती है, जिससे किसी उत्कृष्ट रचना का अर्थ और महत्व नष्ट हो तथा उसके स्थान पर उसके अभीप्सित, उसके गुट के किसी ओछे या निम्नतर पाठ (और इसकी आड़ में उसके लेखक) को प्रतिस्थापित किया जा सके।
खुद सोचिये, एक एक ऐसे जटिल और बहुजन-समाज की संस्कृति, जिसकी सबसे बड़ी विडंबना उसकी लगातार बढ़ती अतिसंवेदी असहिष्णुता, अतिरेकी, हिंस्र और अराजक होती मानसिकता और प्रतिहिंसात्मक वृति है, उसमें आलोचक की यह अतिरंजित निहद्द ‘हाइपरट्रॉफी’, उसका फुफकारता-फुंसेटता, फेंचकुर फेंकता उद्दंड प्रलाप क्या विकल-उन्मादी मस्तिष्क का किसी निहत्थी रचना और उसके पाठ पर लंपट ‘हमला’ नहीं ? ....और उसके द्वारा की जाने वाली ‘व्याख्या’ क्या वही नहीं है, जिसकी शिनाख़्त सुजा़न सोंटाग ने इन शब्दों में की थी -‘ऐसी व्याख्या अतिरेकी बुद्धि द्वारा, रचनात्मक ऊर्जा और ऐंद्रिक संवेदनशीलता की कीमत पर, कला के साथ की गई एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है।’
मैं अपनी कहानियों के इस संचयन के पहले ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी कहानियों के ‘पाठ’ के साथ ही नहीं, स्वयं मेरे निजी जीवन के साथ भी हिंदी की प्राध्यापकीय या सत्ताकेंद्रित आलोचना तथा उनसे अनिवार्य रूप से संबंद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थानों ने यही ‘प्रतिशोधात्मक कार्रवाई’ पिछले कई दशकों से, बार-बार की है। इसके द्वारा उसने रचना के पाठ और उसके अर्थाशयों को क्षतिग्रस्त तो किया ही है, एक नागरिक लेखक के बतौर उसने इन कहानियों के लेखक को एक गरिमाहीन, सामाजिक-आर्थिक अनिश्चयात्मकताओं से भरे निर्वासन की ओर धकेलने की लगातार कोशिश की है। इसमें वह एक हद तक कामयाब इस मायने में रही है कि उसने इस जीवन की वास्तविक सूचनाओं को अपनी सामूहिक-सांगठनिक ताकत के ज़रिये या तो सेंसर किया है या उन्हें अफवाहों से विस्थापित किया है। मेरी ही एक कविता की पंक्ति है-‘जो यथार्थ को व्यक्त करता है, वह मार दिया जाता है अफवाहों से।’
अगर आप मेरी कहानियों-कविताओं और उनसे संबंधित हिंदी की आलोचना आदि से परिचित हैं तो ‘टेपचू’ और ‘तिरिछ’ जैसी प्रारंभिक कहानियों से लेकर ‘वारेन हेंटिंग्स का सांड’, ‘पॉल गोमरा का स्कूटर’, ‘और अंत में प्रार्थना’ जैसी बीच की, और ‘पीली छतरी वाली लड़की’, ‘मोहन दास’ और ‘दिल्ली की दीवार’ या ‘मैंगोसिल’ जैसी हाल-फिलहाल की कहानियों-लघु-उपन्यासों को लेकर हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में आलोचकों-संपादकों द्वारा चलाये गये ‘विवादों’ से भी परिचित होंगे। उन विवादों के स्तर और उनके ‘मकसद’ को लेकर, या उनके पीछे उपस्थित सत्ता-केंद्रों के बारे में मैं अलग से कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यहां मुझे अपने प्रिय और अत्यंत प्रतिभाशाली आलोचक वाल्टर बेंजमिन की फिर याद आती है, जिन्होंने ‘कहानीकार’ शीर्षक से अपने प्रिय कथाकार निकोलोइ लेस्कोव (The Storyteller:Reflections on the works of Nikoloi Leskov) के बहाने किसी किस्सागो की रचना और उसके जीवन में आने वाले संकटों-चुनौतियों का गंभीर और अविस्मरणीय विश्लेषण किया था।
बीसवीं सदी में, प्रथम विश्युवद्ध की हिंसा और अमानवीय विभीषिका में से होकर और बचकर जो लेखक लौटा था, उसके आत्मानुभव इतने आक्रांत करने वाले थे कि वह स्वयं को लंबे समय तक ‘निर्वाक्’ पाता रहा। उसके भीतर यह आशंका निरंतर थी कि वे ताकतें जो उस हिंसा और संहार में सम्मिलित थीं, वे प्रच्छन्न रूप से संस्कृति और समाज में, हार या जीत से अलहदा, ज्यों की त्यों मौज़ूद हैं।
आप स्वयं सोचिये बेंजामिन यह तब लिख रहे थे, जब यूरोप में नाजीवाद मानवता को दूसरे विश्वयुद्ध की ओर धकेल रहा था। वहां का नस्लवाद, जो किसी भी मायने में हमारे देश के जातिवाद और सांप्रदायिकता से कमतर नहीं है, बीसवीं सदी के मध्य में जिस भय और आतंक को रच रहा था, उसमें बेंजमिन जैसे अत्यंत संवेदनशील कला-चिंतक की पहली चिंता यही थी कि ‘क्या अब कोई कथाकार कहानी में सच लिखने का साहस दिखा पाएगा? क्या कहानी अपने अंत के कगार तक पहुंच गई है? हमें अब (अपने समय की) कहानी कहने वाले कथाकार कम से कम क्यों दिखते हैं? वह जो अब से कुछ समय पहले तक हमसे अविच्छिन्न था, उसे हमसे अचानक किसने छीन लिया है?’
जब मैं अपनी कहानियों और जीवन के बारे में सोचता हूं, तो वाल्टर बेंजमिन का निबंध अक्सर याद आता है।
मुझे खुशी यही है कि पाठकों ने, जिनमें हिंदी ही नहीं अन्य भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के पाठक बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं, मेरी रचनाओं को अपनाया। अन्य भाषाओं के विद्वानों और वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त आलोचकों-विचारकों ने भी इन रचनाओं को महत्व और अपूर्व सम्मान दिया। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जिन रचनाओं के कारण हिंदी सत्ता-केंद्रों और प्रतिष्ठानों ने, जातीय तथा राजनीतिक पूर्वग्रहों के चलते, मुझे प्रताड़ना, लांछनाएं और कष्टप्रद ओछे विवाद दिये, उन्हीं रचनाओं के अन्य भाषाओं में अनुवादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिली।
मैंने इस संग्रह में जान-बूझ कर उन कहानियों को भी सम्मिलित किया है, जिनकी ‘व्याख्याएं’ अनेक रूपों में हिंदी की प्रचलित आलोचना में आपको यहां-वहां मिलेंगी। अब इस संकलन के माध्यम से आपके पास उन कहानियों का मूल ‘पाठ’ है, आप स्वयं इस पर अपना मत देंगे।
कहानी एक ऐसी जनप्रिय कला है, जिस पर समय-समय की तमाम सत्ताओं द्वारा लगाए गये अभियोगों पर अंतिम फैसला, पाठकों की ‘जन-अदालत’ ही देती है।
तो आपके कठघरे में अपनी दस प्रिय कहानियों को खड़ा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है आप इस चयन को पसंद करेंगे।
Wednesday, August 18, 2010
नये कहानी संकलन की भूमिका :
पाठ से पहले एक पूर्व-पीठिका
यह निर्णय ले पाना सचमुच बहुत कठिन है कि अब तक, लगभग तीन दशकों के कालखंड में लिखी जा चुकीं बहुत-सी कहानियों में से, अपनी कौन-सी दस कहानियां सबसे अधिक प्रिय हैं ?
सबसे पहली बात तो यही कि किसी भी लेखक द्वारा सारी कहानियां एक साथ, एक ही समय में, एक जैसी स्थितियों-परिस्थितियों में नही लिखी जातीं। हर कहानी के जन्म या निर्माण की अपनी अलग कथा होती है। हर कहानी अलग-अलग समय और यथार्थ की कोख से पैदा होती है और फिर अपना एक अलग जीवन जीती है। सिर्फ इस प्रकट संयोग और प्रमाण के चलते कि इन कहानियों को लिखने वाला कथाकार कोई एक व्यक्ति है, सभी कहानियों की अपनी अलग विशिष्ताओं, भिन्नताओं, चरित्र और निजताओं को सपाट नहीं किया जा सकता।
आलोचना अक्सर ऐसा करती है क्योंकि उसका ध्यान लंबे समय से रचनाकेंद्रित नहीं रहा। वह एक खास तरह की व्यवहारमूलक गड़बड़ी और प्रचलन से ग्रस्त रही है। जब पश्चिम के एक आलोचक ने अपना बहुपठित और बहुचर्चित निबंध-‘लेखक की मृत्यु’ (दि डेथ ऑफ दि ऑथर) लिखा तो उसने यही संकेत देने की पहली कोशिश की थी कि किसी रचना की आलोचना और व्याख्या के लिए उसके लेखक के संस्मरण, डायरी, जीवनी या उसके वैयक्तिक-सामाजिक संदर्भों से जुटाए गये साक्ष्य रचना को समझने में बहुत उपयोगी नहीं होते। क्योंकि लेखक और उसकी हर रचना के बीच हमेशा एक विभाजक रेखा खिंची होती है, भले ही वे किसी दिक् और काल की एक ही सरल रेखा में उपस्थित हों। ‘लेखक अपनी किताब का व्यतीत होता है। उसके और उसकी किताब के बीच ‘पहले’ (पूर्व) और ‘बाद’ (पश्चात) की हमेशा एक रेखा होती है। लेखक अपनी किताब से पहले उसी तरह जीवित रहता है, जिस तरह कोई पिता अपनी संतति के पहले जीवित होता है।’
जाहिर है संतान का जीवन उसके पिता का जीवन नहीं होता। दोनों अपना पृथक और भिन्न जीवन जीते हैं। और जिस तरह किसी संतान का जन्म या भ्रूण में उसका प्रतिस्थापन किसी पिता (या मां) की ‘अभिव्यक्ति’ नहीं बल्कि एक ‘प्रक्रिया’ या ‘कर्म’ है, उसी तरह लेखन का कर्म भी सिर्फ कोई ‘अभिव्यक्ति’ नहीं है। लेखक के हाथ गणेश और उसका सिर (मस्तिष्क) व्यास नहीं हैं, जहां कोई एक बोल रहा है और एक दूसरा लिख रहा है।
इसीलिए उस आलोचक-विचारक ने माना था कि रचना के पाठ का जन्म किसी ‘रिकॉर्डिंग’, ‘नोटेशन’ या ‘टाइपिंग’ की तरह नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आज का रचनाकार लिखे जाने की तात्कालिक, त्वरित, नश्वर, स्फूर्त, क्षणभंगुर प्रक्रिया में रचना के पाठ के साथ ही, उसी पल में जन्म लेता है और ‘पाठ’ के पूरा होते ही, खत्म हो जाता है।
इसके बाद का उसका जीवन उत्तर-पाठ का अलग जीवन है। पाठ के पहले और बाद के उसके जीवन का रचना से पृथक् अर्थ और संदर्भ है। किसी रचना के पाठ का बनना उसी क्षण उसके लेखक का स्थगन और उसकी अनुपस्थिति है। पाठ की उपस्थिति के साथ ही लेखक की विलुप्ति या उसकी अनुपस्थिति तय और मुकम्मल हो जाती है। यह एक तरह से कुछ-कुछ वैसा ही ‘अलगाव’ (एलियनेशन) है, जिसकी चर्चा बीसवीं सदी के प्रमुख मार्क्सवादी विचारकों (जॉर्ज लुकाच आदि) ने औद्योगिक-पूंजीवादी समाज में व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में की है। रचयिता और रचना, हुनरमंद और उत्पाद के बीच का अलगाव। श्रमिक और उसकी रचना के बीच का अलगाव।
हमारी हिंदी भाषा में आलोचना अभी तक विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में ही डगमग करती दिख रही है और इसका खामियाजा इस समय लिखी जा रही नयी रचनाओं को भुगतना पड़ता है। यह आलोचना किसी भी रचना को किसी व्यक्ति (लेखक) की अभिव्यक्ति या उसके विचार का ‘भाष्य’ अथवा ‘संप्रेषण’ मानते हुए, पाठ को छोड़ कर लेखक की गर्दन पकड़ लेती है। ऐसी आलोचना की व्याख्या या दुर्व्याख्या से रचना के पाठ की क्षति जितनी होती है, उससे अधिक उस व्यक्ति की हो जाती है, जो निर्दिष्ट संयोग से उस पाठ की निर्मिति के पूर्व उसका ‘लेखक’ हुआ करता था। रचना पीछे रह जाती है क्योंकि उसके पाठ को ‘पाठक’ की स्मृतियां और उनकी प्रज्ञाएं तो बचा लेती हैं, उत्पीड़न असल में लेखक का होने लगता है। किसी विकलांग ‘विकल-मस्तिष्क’ (एक अननुपातिक, असंयमित और अनैतिक विभ्रांत गुटबाज लेखक का 'पद'-'जनसत्ता' से उद्धृत) वाली आलोचना की तानाशाही के दौर में किसी लेखक का जीवन उस सूफी या संत जैसा होता है, जिसके पद और साखियों को तो सचेत जन-समुदाय बचा लेता है, लेकिन उस पाठ के रचनाकार की नियति उसे किसी मकतल या सलीब की दिशा की ओर ही अक्सर ले जाती अब तक इतिहास में दिखी है। हिंदी समाज में जितनी जातीयताएं, अस्मिताएं, वर्ग और उनसे संबद्ध जितनी तरह की राजनीतिक सत्ता-संरचनाएं हैं, उसके चलते लेखक और पाठ का संकट और गहरा हो जाता है। मैंने इसीलिए, समय-समय पर, मौका मिलते ही, सुजा़न सोंटाग, मुक्तिबोध या रोलां बाथ के विचारों का हवाला दिया है।
आप आज के समूचे समकालीन साहित्यिक परिदृश्य को देखिए। आत्मकथाओं, साक्षात्कारों, वक्तव्यों, डायरियों, संस्मरणों, आरोपों-प्रत्यारोपों से सब कुछ अंटा पड़ा है। कवि डायरियां लिख रहे हैं, कथाकार आत्मकथाएं और संस्मरण, जैसे उनका यह कर्म उनकी रचनाओं की ही निरंतरता का कोई जैविक-भौतिक साक्ष्य और सबूत हो। जब कि लिखना भाषा के भीतर घटित और संपन्न होती एक ऐसी प्रक्रिया या कर्म है जिसकी शुरूआत के पहले क्षण के साथ ही उस भाषा के समस्त कूटों, संकेतों, प्रतीकों के सभी बाहरी उद्गम-सूत्रों का विनाश शुरू हो जाता है। किसी भी रचना का भाषिक पाठ उस भाषा के बाहरी सूत्रों से उसके पृथक होने का, स्वतंत्र और मुक्त होने का पहला प्रमाण है। अगर ऐसा नहीं है, तो वह रचना अपने अनिवार्य एस्थेटिक्स में, रचना हो पाने से चूक जाती है।
(हांलाकि ऐसे समय में अपनी किसी आने वाली किताब की ऐसी भूमिका लिखना सत्ता और महत्वाकांक्षाओं के उन्माद में ग्रस्त सत्ता-समाज के 'कौरव-कोहराम' या 'कुरु-कलरव' के बीच एक विगलित-विचलित हो चुके अकेले लेखक की 'फुसफुसाहट' से अधिक कुछ नहीं है, फिर भी इसका अगला बाकी हिस्सा कल या परसों आप यहां देखेंगे। यह भूमिका 'किताब घर' प्रकाशन से शीघ्र आने वाली किताब 'मेरी प्रिय दस कहानियां' का पहला तात्कालिक अंश है।)
यह निर्णय ले पाना सचमुच बहुत कठिन है कि अब तक, लगभग तीन दशकों के कालखंड में लिखी जा चुकीं बहुत-सी कहानियों में से, अपनी कौन-सी दस कहानियां सबसे अधिक प्रिय हैं ?
सबसे पहली बात तो यही कि किसी भी लेखक द्वारा सारी कहानियां एक साथ, एक ही समय में, एक जैसी स्थितियों-परिस्थितियों में नही लिखी जातीं। हर कहानी के जन्म या निर्माण की अपनी अलग कथा होती है। हर कहानी अलग-अलग समय और यथार्थ की कोख से पैदा होती है और फिर अपना एक अलग जीवन जीती है। सिर्फ इस प्रकट संयोग और प्रमाण के चलते कि इन कहानियों को लिखने वाला कथाकार कोई एक व्यक्ति है, सभी कहानियों की अपनी अलग विशिष्ताओं, भिन्नताओं, चरित्र और निजताओं को सपाट नहीं किया जा सकता।
आलोचना अक्सर ऐसा करती है क्योंकि उसका ध्यान लंबे समय से रचनाकेंद्रित नहीं रहा। वह एक खास तरह की व्यवहारमूलक गड़बड़ी और प्रचलन से ग्रस्त रही है। जब पश्चिम के एक आलोचक ने अपना बहुपठित और बहुचर्चित निबंध-‘लेखक की मृत्यु’ (दि डेथ ऑफ दि ऑथर) लिखा तो उसने यही संकेत देने की पहली कोशिश की थी कि किसी रचना की आलोचना और व्याख्या के लिए उसके लेखक के संस्मरण, डायरी, जीवनी या उसके वैयक्तिक-सामाजिक संदर्भों से जुटाए गये साक्ष्य रचना को समझने में बहुत उपयोगी नहीं होते। क्योंकि लेखक और उसकी हर रचना के बीच हमेशा एक विभाजक रेखा खिंची होती है, भले ही वे किसी दिक् और काल की एक ही सरल रेखा में उपस्थित हों। ‘लेखक अपनी किताब का व्यतीत होता है। उसके और उसकी किताब के बीच ‘पहले’ (पूर्व) और ‘बाद’ (पश्चात) की हमेशा एक रेखा होती है। लेखक अपनी किताब से पहले उसी तरह जीवित रहता है, जिस तरह कोई पिता अपनी संतति के पहले जीवित होता है।’
जाहिर है संतान का जीवन उसके पिता का जीवन नहीं होता। दोनों अपना पृथक और भिन्न जीवन जीते हैं। और जिस तरह किसी संतान का जन्म या भ्रूण में उसका प्रतिस्थापन किसी पिता (या मां) की ‘अभिव्यक्ति’ नहीं बल्कि एक ‘प्रक्रिया’ या ‘कर्म’ है, उसी तरह लेखन का कर्म भी सिर्फ कोई ‘अभिव्यक्ति’ नहीं है। लेखक के हाथ गणेश और उसका सिर (मस्तिष्क) व्यास नहीं हैं, जहां कोई एक बोल रहा है और एक दूसरा लिख रहा है।
इसीलिए उस आलोचक-विचारक ने माना था कि रचना के पाठ का जन्म किसी ‘रिकॉर्डिंग’, ‘नोटेशन’ या ‘टाइपिंग’ की तरह नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आज का रचनाकार लिखे जाने की तात्कालिक, त्वरित, नश्वर, स्फूर्त, क्षणभंगुर प्रक्रिया में रचना के पाठ के साथ ही, उसी पल में जन्म लेता है और ‘पाठ’ के पूरा होते ही, खत्म हो जाता है।
इसके बाद का उसका जीवन उत्तर-पाठ का अलग जीवन है। पाठ के पहले और बाद के उसके जीवन का रचना से पृथक् अर्थ और संदर्भ है। किसी रचना के पाठ का बनना उसी क्षण उसके लेखक का स्थगन और उसकी अनुपस्थिति है। पाठ की उपस्थिति के साथ ही लेखक की विलुप्ति या उसकी अनुपस्थिति तय और मुकम्मल हो जाती है। यह एक तरह से कुछ-कुछ वैसा ही ‘अलगाव’ (एलियनेशन) है, जिसकी चर्चा बीसवीं सदी के प्रमुख मार्क्सवादी विचारकों (जॉर्ज लुकाच आदि) ने औद्योगिक-पूंजीवादी समाज में व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में की है। रचयिता और रचना, हुनरमंद और उत्पाद के बीच का अलगाव। श्रमिक और उसकी रचना के बीच का अलगाव।
हमारी हिंदी भाषा में आलोचना अभी तक विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में ही डगमग करती दिख रही है और इसका खामियाजा इस समय लिखी जा रही नयी रचनाओं को भुगतना पड़ता है। यह आलोचना किसी भी रचना को किसी व्यक्ति (लेखक) की अभिव्यक्ति या उसके विचार का ‘भाष्य’ अथवा ‘संप्रेषण’ मानते हुए, पाठ को छोड़ कर लेखक की गर्दन पकड़ लेती है। ऐसी आलोचना की व्याख्या या दुर्व्याख्या से रचना के पाठ की क्षति जितनी होती है, उससे अधिक उस व्यक्ति की हो जाती है, जो निर्दिष्ट संयोग से उस पाठ की निर्मिति के पूर्व उसका ‘लेखक’ हुआ करता था। रचना पीछे रह जाती है क्योंकि उसके पाठ को ‘पाठक’ की स्मृतियां और उनकी प्रज्ञाएं तो बचा लेती हैं, उत्पीड़न असल में लेखक का होने लगता है। किसी विकलांग ‘विकल-मस्तिष्क’ (एक अननुपातिक, असंयमित और अनैतिक विभ्रांत गुटबाज लेखक का 'पद'-'जनसत्ता' से उद्धृत) वाली आलोचना की तानाशाही के दौर में किसी लेखक का जीवन उस सूफी या संत जैसा होता है, जिसके पद और साखियों को तो सचेत जन-समुदाय बचा लेता है, लेकिन उस पाठ के रचनाकार की नियति उसे किसी मकतल या सलीब की दिशा की ओर ही अक्सर ले जाती अब तक इतिहास में दिखी है। हिंदी समाज में जितनी जातीयताएं, अस्मिताएं, वर्ग और उनसे संबद्ध जितनी तरह की राजनीतिक सत्ता-संरचनाएं हैं, उसके चलते लेखक और पाठ का संकट और गहरा हो जाता है। मैंने इसीलिए, समय-समय पर, मौका मिलते ही, सुजा़न सोंटाग, मुक्तिबोध या रोलां बाथ के विचारों का हवाला दिया है।
आप आज के समूचे समकालीन साहित्यिक परिदृश्य को देखिए। आत्मकथाओं, साक्षात्कारों, वक्तव्यों, डायरियों, संस्मरणों, आरोपों-प्रत्यारोपों से सब कुछ अंटा पड़ा है। कवि डायरियां लिख रहे हैं, कथाकार आत्मकथाएं और संस्मरण, जैसे उनका यह कर्म उनकी रचनाओं की ही निरंतरता का कोई जैविक-भौतिक साक्ष्य और सबूत हो। जब कि लिखना भाषा के भीतर घटित और संपन्न होती एक ऐसी प्रक्रिया या कर्म है जिसकी शुरूआत के पहले क्षण के साथ ही उस भाषा के समस्त कूटों, संकेतों, प्रतीकों के सभी बाहरी उद्गम-सूत्रों का विनाश शुरू हो जाता है। किसी भी रचना का भाषिक पाठ उस भाषा के बाहरी सूत्रों से उसके पृथक होने का, स्वतंत्र और मुक्त होने का पहला प्रमाण है। अगर ऐसा नहीं है, तो वह रचना अपने अनिवार्य एस्थेटिक्स में, रचना हो पाने से चूक जाती है।
(हांलाकि ऐसे समय में अपनी किसी आने वाली किताब की ऐसी भूमिका लिखना सत्ता और महत्वाकांक्षाओं के उन्माद में ग्रस्त सत्ता-समाज के 'कौरव-कोहराम' या 'कुरु-कलरव' के बीच एक विगलित-विचलित हो चुके अकेले लेखक की 'फुसफुसाहट' से अधिक कुछ नहीं है, फिर भी इसका अगला बाकी हिस्सा कल या परसों आप यहां देखेंगे। यह भूमिका 'किताब घर' प्रकाशन से शीघ्र आने वाली किताब 'मेरी प्रिय दस कहानियां' का पहला तात्कालिक अंश है।)
Subscribe to: Posts (Atom)
'मोहन दास' अब विद्यापति और बाबा नागार्जुन की भाषा में
Warren Hastings kaa Sand' Translated in Hungarian
भारतीय गणराज्य के लोग 'राष्ट्र' होने से क्यों डरते हैं?
'पीली छतरी वाली लड़की' अब मलयालम की विख्यात पत्रिका 'देशाभिमानी' में धारावाहिक

प्रो. सन्नी एन.एम., क्रिश्चियन कालेज, मलाबार, कालीकट का अनुवाद
'पीली छतरी वाली लड़की' के जर्मन अनुवाद को अपूर्व सफ़लता : अमेज़ान पर ५ सितारे
Watch Mohan Das online
30 South Asian Youth Icons
हिंसा और अहिंसा से हट कर
पीली छतरी वाली लड़की अब मराठी में

अनुवाद: चर्चित युवा समकालीन मराठी कवि और चित्रकार गणेश विसपुते, अगस्त में मुंबई में लोकार्पण
Iliya Trojanov, Uday Prakash and Fatima in Seminar
Welcome to ICORN General Assembly
Delhi My Life
Hindu Fascism cuts across Political and Ideological lines
अपने निर्दोष पड़ोसियों को मृत्यु के पंजों से बचाने के लिए आवाज़ उठाएं
Life and Struggles at the fringe
दिल्ली की दीवार
सार्क देशों का जन-समाज नस्ल, धर्म, जाति में यूरोप जैसा एक वचन नहीं है
पीली छतरी वाली लड़की: एक अनोखी प्रेम कथा
मो्हन दास अब मराठी में उपलब्ध अनुवाद वनिता सावंत

लोक वांग्मय गृह, भूपेश गुप्ता भवन, प्रभादेवी रोड, मुंबई द्वारा प्रकाशित
दि क्वार्टरली कनवर्सेशन में 'पीली छतरी वाली लडकी' पर जेसन का साक्षात्कार
Best South Asia Books of the 2000s
जाति, लिंग और वर्ग से परे कोई 'आइडेंटिटी' नहीं होती
हिंदुस्तान टाइम्स में 'दिल्ली नायर' पर टिप्पणी
Amnesty International
कागद कारे : रेडियो कार्यक्रम
Columbus in Our Times
Writing Hindi in Globalizing World
Between the Lines
Dilli ki Deewaar
Doctor Wakankar : Readings and Discussions
The Girl with Golden Parasol in Bonn
मोहन दास फिल्म पर अखबारों की राय
The Politics of Lying and Culture of Deceit
Struggle for Language, Land and Literature
'पीली छतरी वाली लड़की' इसी अक्टूबर में जर्मनी में
अपनी खोई हुई पहचान कहां से लाऊं
युद्ध के विरुद्ध उठा हुआ हाथ
Slum Dog का जवाब है Delhi noir :
Delhi noir arrives in India / खुश खबरी

HarperCollins launches award winning publication in August. 'दिल्ली की दीवार' अब आएगी दिल्ली,'
डाक्टर वाकणकर : 'और अंत में प्रार्थना' का जर्मन अनुवाद

Translated in to German by Andre Penz. Will be released on 14th Oct.2009 at World Book Fair, Frankfurt. Publisher: Draupadi Verlag, Heidelberg, Germany.
“Delhi noir” means the achievement of a style
Tehelka talks about Delhi Noir
'दिल्ली की दीवार' अभिनेता अजय नायडू का पाठ
Words and War
मुकुल शिवपुत्र को सृजन का शरण्य
Delhi noir being launched on 10th June in New York
Yangesh: Who took Mohan Das to Nepal, speaks.
English vs Hindi : Post-colonial Perspective : Caste and Class Clashes
Delhi Noir में 'दिल्ली की दीवार'
.jpg)
Akashic Books, New York : Edited by Hirsh Sawhney. Authors : Allan Sealy, Meera Nair, Omair Ahmed, Ruchir Joshi, Radhika Jha, Manjula Padmnabhan, Uday Prakash and few more. DELHI NOIR’S FOURTEEN ORIGINAL STORIES are written by the best Indian writers alive today—the ones you haven’t yet heard of but should have. They are veteran authors who have appeared on the Booker Prize short list and budding geniuses who your grandchildren will read about in English class. Delhi Noir is a world of sex in parks, male prostitution, and vigilante rickshaw drivers. It is one plagued by religious riots, soulless corporate dons, and murderous servants. This is India uncut, the one you’re missing out on because mainstream publishing houses and glossy magazines can’t stomach it.
People's Watch : Monitoring TV Monitor
लेखक की मृत्यु अभी बाकी है
Reading of 'The Girl with the Golden Parasol' at ALTA
व्योम मे शब्द
International Literature Seminar in Republic of Korea
हेराल्ड पिंटर को श्रद्धांजलि
वारेन हेस्टिंग्स का सांड
मोहन दास की एक समीक्षा ये भी है :
मोहनदास पर मिहिर की राय
मोहनदास का अपहरण और भ्रष्ट पूंजी की नयी ताकत
A new Feature Film is coming up soon.
Mohan Das in more languages
Mohan Das up to now has been translated in :
1. English : by Pratik Kanjilal, a brilliant and young translator, Sahitya Akademi award winner for translating Nirmal Verma's Antim Aranya. He is editor of most reputed literary journal 'Little Magazine'.
2. Oriya : by well known poet and writer Manu Dash. Mohan Das in Oriya will be out by Deewali seasons.
3. Urdu : by Hyder Jafri Syed, a most gifted translator, also a Sahitya Akademi award winner in translations.
4.Kannada : by R.P. Hegde, a well known Kannada writer and translator. The book is in prints at Banglore.
5. Punjabi : by Rabinder Singh Bath, a senior and most revered translator. He has been known for translating Bhisma Sahani's novel Tamas in Punjabi.
6. Marathi : by Vanita Savant, a well known translator. Famous for translating Vijaidan Detha's Rajasthani Literary classic 'Duvidha aur anya kahaniyan'.
7. Nepali : by Yagyesh, a young writer with the background of science, residing in Nepal.
8.Telugu : by Venugopalan, renowned writer and Civil Right activist of Andhra Pradesh.
1. English : by Pratik Kanjilal, a brilliant and young translator, Sahitya Akademi award winner for translating Nirmal Verma's Antim Aranya. He is editor of most reputed literary journal 'Little Magazine'.
2. Oriya : by well known poet and writer Manu Dash. Mohan Das in Oriya will be out by Deewali seasons.
3. Urdu : by Hyder Jafri Syed, a most gifted translator, also a Sahitya Akademi award winner in translations.
4.Kannada : by R.P. Hegde, a well known Kannada writer and translator. The book is in prints at Banglore.
5. Punjabi : by Rabinder Singh Bath, a senior and most revered translator. He has been known for translating Bhisma Sahani's novel Tamas in Punjabi.
6. Marathi : by Vanita Savant, a well known translator. Famous for translating Vijaidan Detha's Rajasthani Literary classic 'Duvidha aur anya kahaniyan'.
7. Nepali : by Yagyesh, a young writer with the background of science, residing in Nepal.
8.Telugu : by Venugopalan, renowned writer and Civil Right activist of Andhra Pradesh.
ओ हेनरी कथा सम्मान २००८
तहलका का कहना है.....
शिकागो मे समारोह्
Acidic Margins of an Author's Life
पीली छतरी वाली लड़्कीः अमेरिका में

शिकागो विश्वविद्यालय में समारोह 'Uday Prakash's stories are fables about survival amid the forces that have legislated extinction for all-Amitava Kumar (Author of 'Husband of a Fanatic',and 'Passport Photos')
The Girl with the Golden Parasol
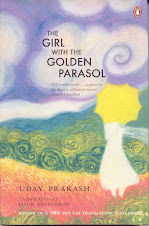
Translated by Jason Grunebaum, Winner of a 2005 PEN USA Translation Fund Award '' A terrific novel....a paean to the dignity of human desires'' -Amit Chaudhury (author of 'Freedom Song' and 'Afternoon Raag')
'Daddu Tiwari'' in English by Robert A. Hueckstedt
वारेन हेस्टिंग्स का सांड
Fiction
| Slice of history in modern times |  |  |  |
| Written by Tribune News Service, Chandigarh | |
| Thursday, 14 February 2008 | |
 The department of Indian theatre is ready with its annual production and this time it is history vis-à-vis modern times. The play titled ‘Warren Hastings ka saand’ is based on a short story written by writer Uday Prakash by the same name. The play portrays various aspects of exploitation, be it at the hands of the Britishers in the past or Indians at the hands of fellow Indians in the present. The department of Indian theatre is ready with its annual production and this time it is history vis-à-vis modern times. The play titled ‘Warren Hastings ka saand’ is based on a short story written by writer Uday Prakash by the same name. The play portrays various aspects of exploitation, be it at the hands of the Britishers in the past or Indians at the hands of fellow Indians in the present.Directed by Kumara Varma of the department, the story revolves around Warren Hastings who comes to India and adapts the culture and later on succumbs to the system and becomes what the system wants him to be. “The idea is to show that in some form or the other the exploitation continues even after India being independent. Sometimes it is in the form of capitalism, sometimes globalisation and at times when the outside forces capture our markets. But it’s the common man who suffers ultimately”, said one of the actors. Lord Clive had observed what was happening in the contemporary times more than 200 years ago and his observations were depicted through a powerful speech in the play”, said another. To make it a success, the students are researching, rehearsing and doing everything related to the play themselves from costume designing to lights arranging. |
एक भाषा हुआ करती है
Incredible India... Just watch it
Language is Means of Existence
Native Wood Carvers of US
News in a click
CNET
- Jul 09, 2011
- 5 hours ago
by Josh Lowensohn The first of the big name e-book reading apps has removed links to its external e-bookstore in order to conform with Apple's recently-implemented App Store policy. Borders, which has has had its e-book offering on the App Store for ...
Apple Insider
- Jul 09, 2011
- 6 hours ago
By Josh Ong A Brooklyn-based artist is being investigated by Apple and the Secret Service after installing spy camera software on New York Apple Retail Store computers that took pictures of customers and sent them to a remote server. ...
Digitaltrends.com
- Jul 09, 2011
- 6 hours ago
Rumor has it that Apple will release a high-end "iPad HD" with a 2048x1536 resolution display this fall. The Apple rumor mill ramped up to full speed this week with reports that Apple has a new iPad model set for release this fall. ...
Register
- Jul 09, 2011
- 11 hours ago
One day, if Apple follows through on work embodied in a recent patent application, you'll be able to "pour" data from your iPhone into an iPad lying on a table below it. Or, with the flick of the wrist, you'll "throw" photos and videos from from your ...
powered by |  |
Blog Archive
- Mar 02 (1)
- Jan 16 (1)
- Oct 10 (1)
- Sep 20 (1)
- Sep 10 (1)
- Aug 27 (1)
- Aug 18 (1)
- Jul 21 (1)
- Jun 01 (1)
- May 23 (1)
- May 14 (1)
- May 03 (1)
- May 01 (1)
- Apr 25 (1)
- Apr 19 (1)
- Apr 18 (1)
- Apr 09 (1)
- Apr 07 (1)
- Apr 06 (1)
- Jan 19 (1)
- Jan 16 (1)
- Jan 12 (1)
- Dec 14 (1)
- Dec 10 (1)
- Oct 14 (1)
- Oct 06 (1)
- Sep 28 (1)
- Sep 06 (1)
- Aug 28 (1)
- Aug 23 (1)
- Aug 02 (1)
- Jul 29 (1)
- Jul 20 (1)
- Jul 16 (1)
- Jul 13 (1)
- Jul 12 (2)
- Jul 11 (1)
- Jul 09 (1)
- Jun 26 (1)
- Jun 24 (1)
- Jun 15 (1)
- Jun 08 (1)
- Jun 03 (1)
- May 31 (1)
- May 27 (1)
- May 09 (1)
- May 08 (1)
- May 03 (1)
- May 01 (2)
- Apr 30 (1)
- Apr 25 (1)
- Apr 03 (1)
- Mar 29 (1)
- Mar 25 (1)
- Mar 24 (1)
- Mar 21 (1)
- Mar 17 (1)
- Mar 10 (1)
- Mar 02 (1)
- Jan 22 (1)
- Jan 14 (1)
- Dec 26 (1)
- Dec 25 (1)
- Dec 17 (1)
- Nov 29 (1)
- Jul 04 (1)
- Jun 30 (1)
- Jun 27 (1)
- Jun 18 (1)
- Jun 16 (1)
- Jun 14 (1)
- Jun 09 (1)
- Jun 06 (1)
- Jun 03 (1)
- Jun 01 (1)
- May 30 (1)
- May 27 (1)
- May 17 (1)
- May 11 (1)
- May 07 (1)
- May 06 (1)
- May 05 (1)
- May 03 (1)
- Apr 21 (1)
- Apr 18 (1)
- Apr 17 (1)
- Apr 09 (1)
- Apr 02 (1)
- Mar 29 (1)
- Mar 24 (1)
- Mar 22 (1)
- Mar 17 (1)
- Mar 14 (1)
- Feb 28 (1)
- Feb 27 (1)
- Feb 17 (1)
- Feb 11 (1)
- Feb 07 (1)
- Feb 05 (1)
- Feb 02 (1)
- Jan 30 (1)
- Jan 16 (1)
- Jan 15 (1)
- Jan 03 (1)
- Jan 01 (1)
- Dec 30 (2)
- Dec 24 (1)
- Dec 22 (1)
- Dec 21 (1)
- Dec 20 (1)
- Dec 04 (1)
- Nov 16 (1)
- Nov 12 (1)
- Nov 10 (1)
- Nov 04 (1)
- Oct 30 (2)
- Oct 28 (1)
- Oct 10 (1)
- Oct 07 (1)
- Oct 06 (1)
- Oct 02 (1)
- Sep 25 (1)
- Sep 21 (1)
- Sep 20 (1)
- Sep 18 (1)
- Sep 11 (1)
- Sep 09 (1)
- Sep 08 (1)
- May 07 (1)
- Apr 22 (1)
- Apr 18 (2)
- Apr 16 (1)


























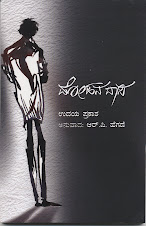






कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें